‘ आमि सेइ दिन होबो शांत,
आमि सेइ दिन होबो शांत,
 आमि सेइ दिन होबो शांत,
आमि सेइ दिन होबो शांत,जबे उत्पीड़ितेर क्रंदन-रोल आकाशे बातासे ध्वनिबे ना, अत्याचारीर खड्ग कृपाण भीम रणभूमे रनिबे ना।’
(मै उसी दिन हूंगा शांत,
जब उत्पीड़ितों का करुण क्रंदन गगन पवन में न गूंजेगा,
अत्याचारी के खड्ग, कृपाण भयंकर रणभूमि में नहीं झनझनायेंगे)
उक्त पंक्तियाँ बांग्ला के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम द्वारा 1922 में रचित प्रसिद्ध कविता ‘प्रलयोल्लास’ की हैं. हालांकि इसके आधारभूत प्रेरणा का केन्द्र वो वामपंथ की सैद्धांतिकी है जो एक समय वंचितों-शोषितों की आतंरिक पीड़ा की त्वरा का भेरीनाद बनी जो अपने उत्थान के युग में विश्वभर के पददलित वर्ग के परिवर्तन की उम्मीद की संवाहक बनी. ये पहली बार था कि शोषित-वंचित वर्ग को वामपंथ-मार्क्सवाद की आवाज में अपने लिए राजनीतिक-सामाजिक चेतना की त्वरा महसूस हुईं.
लेकिन इतिहास की नियति का निर्णयन में आज यह विचारधारा मौन मृत्यु की ओर अग्रसर है. मृत्यु ही तो है उस राजनीतिक-सामाजिक विचारधारा का जो ना तो अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने में सक्षम है और ना जन चेतना एवं उसकी तवज्जो को अपनी ओर आकर्षित करने में. एक तरफ देश हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के चुनावी तकरार में उलझा था, जहाँ नेताओं के अनर्गल बयानों एवं गैर-जरुरी मुद्दों पर बहस भी चर्चा में थी और उसी समय देश की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी माकपा अपने केन्द्रीय कमेटी की बैठक में सीताराम येचुरी के निधन के बाद उपजे रिक्ति में साम्यवाद का अगला सितारा चुनने की जहद्दोजद में लगी थी.
लेकिन देश के मुख्यधारा के सूचना-तंत्र में इससे जानने में कोई रूचि नहीं थी. हो सकता है कि तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया माध्यमों पर ये आरोप लगा दिया जाये कि वे तो बिकाऊ हैं, वे विज्ञापनजीवी हैं, या वे बाकी पार्टियों से फायदा लेते हैं आदि आदि. लेकिन ये उस नैसर्गिक आलोचना के समक्ष एक प्रकार का छल होगा कि वामपंथी राजनीति तीव्र पतनशीलता के साथ अपने वैचारिक अवसान की ओर अग्रसर है.
वैसे प्रसंगवश ये कहना अनुचित ना होगा कि इस पतनशील राजनीतिक पक्ष का अतीत बड़ा आकर्षक रहा है. 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरी आधुनिक जन चेतना के वैचारिक स्वरों को ठोस आकार तब मिला ज़ब 1917 में रुसी क्रांति हुईं. भारत ने भी उसी दौरान राजशाही एवं औपनिवेशवाद के घुटन और विषाक्त भरी राजनीति में वामपंथ के इस स्वच्छन्द, उन्मुक्त वायु में जीना सीखा. इसमें कोई शक नहीं है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ ने एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा पैदा की. वे जनस्वीकृत, जन प्रशंसित भी हुए. स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रचण्ड जन समर्थन के समक्ष वामपंथी ही सबसे बड़े वैचारिक प्रतिद्वंदी रहें थे.
लेकिन जो सैद्धांतिक शक्ति वामपंथी राजनीति के उत्कर्ष का कारक रहीं, वही अपने रूढ़िवादी स्वरुप में पतन का बायस भी बनी है. आलोचकों की दृष्टि में मार्क्सवाद मूलतः जड़वादी है और उससे भी अधिक अर्थवादी है. अतः उसके चेतन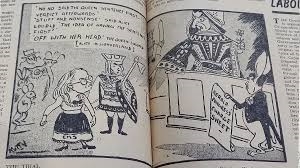 की व्याख्या भी जड़ आधारित एवं धर्म की अर्थ से होती है. यह भी सही है कि भौतिक जीवन के संघर्षों के कारण अभौतिक क्षेत्र में तलाशना तथा उनके विस्तार के लिए उपाय आध्यात्मिक क्षेत्र में ढूंढना भी अनुचित है लेकिन धर्म और अर्थ के प्रतिमान एक विस्तृत अवधारणा है, दूसरे तत्व एवं दर्शन की व्याख्याएं देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हैं. लेकिन भारतीय वामपंथियों के पास अपनी ही वैचारिक हठधार्मिता है. जैसे मार्क्स को मानवता मानव के श्रम में ही दिखाई दी वैसे ही उनके भारतीय अनुयायियों को किताबी कुतर्कों में. वे भारत की स्थानीय परिस्थितियों में धर्म, अर्थ और सामाजिक संरचना को समझें बगैर अपने सैद्धांतिक ज्ञान में ही डूबे रहें.
की व्याख्या भी जड़ आधारित एवं धर्म की अर्थ से होती है. यह भी सही है कि भौतिक जीवन के संघर्षों के कारण अभौतिक क्षेत्र में तलाशना तथा उनके विस्तार के लिए उपाय आध्यात्मिक क्षेत्र में ढूंढना भी अनुचित है लेकिन धर्म और अर्थ के प्रतिमान एक विस्तृत अवधारणा है, दूसरे तत्व एवं दर्शन की व्याख्याएं देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हैं. लेकिन भारतीय वामपंथियों के पास अपनी ही वैचारिक हठधार्मिता है. जैसे मार्क्स को मानवता मानव के श्रम में ही दिखाई दी वैसे ही उनके भारतीय अनुयायियों को किताबी कुतर्कों में. वे भारत की स्थानीय परिस्थितियों में धर्म, अर्थ और सामाजिक संरचना को समझें बगैर अपने सैद्धांतिक ज्ञान में ही डूबे रहें.
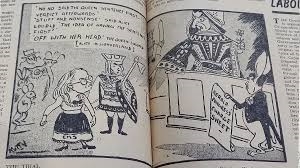 की व्याख्या भी जड़ आधारित एवं धर्म की अर्थ से होती है. यह भी सही है कि भौतिक जीवन के संघर्षों के कारण अभौतिक क्षेत्र में तलाशना तथा उनके विस्तार के लिए उपाय आध्यात्मिक क्षेत्र में ढूंढना भी अनुचित है लेकिन धर्म और अर्थ के प्रतिमान एक विस्तृत अवधारणा है, दूसरे तत्व एवं दर्शन की व्याख्याएं देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हैं. लेकिन भारतीय वामपंथियों के पास अपनी ही वैचारिक हठधार्मिता है. जैसे मार्क्स को मानवता मानव के श्रम में ही दिखाई दी वैसे ही उनके भारतीय अनुयायियों को किताबी कुतर्कों में. वे भारत की स्थानीय परिस्थितियों में धर्म, अर्थ और सामाजिक संरचना को समझें बगैर अपने सैद्धांतिक ज्ञान में ही डूबे रहें.
की व्याख्या भी जड़ आधारित एवं धर्म की अर्थ से होती है. यह भी सही है कि भौतिक जीवन के संघर्षों के कारण अभौतिक क्षेत्र में तलाशना तथा उनके विस्तार के लिए उपाय आध्यात्मिक क्षेत्र में ढूंढना भी अनुचित है लेकिन धर्म और अर्थ के प्रतिमान एक विस्तृत अवधारणा है, दूसरे तत्व एवं दर्शन की व्याख्याएं देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हैं. लेकिन भारतीय वामपंथियों के पास अपनी ही वैचारिक हठधार्मिता है. जैसे मार्क्स को मानवता मानव के श्रम में ही दिखाई दी वैसे ही उनके भारतीय अनुयायियों को किताबी कुतर्कों में. वे भारत की स्थानीय परिस्थितियों में धर्म, अर्थ और सामाजिक संरचना को समझें बगैर अपने सैद्धांतिक ज्ञान में ही डूबे रहें.60 और 70 के दशक में इस आंदोलन में दक्षिणपंथी और वामपंथी संशोधनवाद के नाम पर हुईं टूट के बाद रणनीति और कार्यनीति पर मतभेद के कारण इसने निरंतर पतन ही देखा है. जिसका कारण वामपंथ सैद्धांतिक हठवाद ही रहा है. हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात् वामपंथ ने भारतीय राजनीति में कई रूपों में विस्तार का प्रयास किया, कभी वह मार्क्सवाद के रास्ते चला, कभी साम्यवाद-समाजवाद के रास्ते, बल्कि एक समय तो क्रांति स्थापित करने की उत्तेजना में उसने सशस्त्र नक्सलवाद का भी रास्ते चुना लेकिन क्षणिक अग्निकांड जैसी जुगुप्सा पैदा करने के अतिरिक्त उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं रह सका. यानि वे गाँव-शहर के वंचितों-शोषितों से लेकर जंगल के वनवासी समाज तक पहुंचे लेकिन फिर हर जगह से सिमटते गये. आज राज्यों विधानमंडलों से लेकर के लेकर केन्द्र की संसद तक वे जनप्रतिनिधित्व के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गये हैं.
लोकतंत्र की गरिमा संवैधानिक प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शनों से समृद्ध होती है. इस समृद्धि में उक्त दल और विचारधारा की भी समान साझेदारी होती है.दूर न जायें, पिछले एक दशकों की राजनीतिक यात्रा में वामपंथियों की वैचारिक अवसान के प्रमाण दिख जायेंगे. जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन आम भारतीय जनमानस के लिए एक नकारात्मक सन्देश था, लेकिन अग्निवीर, बढ़ता निजीकरण, परीक्षाओं में धांधली जैसे मुद्दों पर आंदोलनविहीन चुप्पी भी समझ से परे रही.
असल में 70 के दशक में सत्ता संरक्षण में सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के वातानुकूलित कमरों में जो व्यवस्था परिवर्तन के ज्ञान गढ़े जाने का दौर शुरू हुआ, वही वास्तव में वामपंथ के चारित्रिक दोमुहेपन और नैतिक अवसान का प्रारंभिक समय था जो बाद में तीव्र होता गया और सड़क के संघर्ष और जनमुद्दों पर आधारित सत्ता के निर्णयों का प्रतिकार करने ला माद्दा ख़त्म होने लगा. यही वह समय था ज़ब वामपंथी दलों की राजनीति कांग्रेसी सत्ता की पिछलग्गू बनी और आज तक कमोबेश यही स्थिति है.
1942 की अगस्त क्रांति में अपने वैचारिक रुख के आम भारतीय समाज में निंदित प्रतिक्रिया को देखने समझने के बाद भी वामपंथी आंदोलन अपना सैद्धांतिक परिष्कार नहीं कर सका उसने 70 के दशक में कांग्रेस के आपातकालवादी सत्ता में अनुशासन पर्व के दर्शन कर फिर से वही. गलती दोहराई और नक्सलवाद के क्रांति कम, लेवी वसूली एवं अतार्किक हत्या और आतंक प्रसार से पुनः अपनी मानसिक मतिभ्रमता साबित की.
 1978 में एक भाकपा नेता ने पार्टी की ग्यारहवीं कांग्रेस में स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की स्वतंत्र भावमूर्ति धूमिल हो गयी थी और लोग उसे तथा तत्कालीन शासक को एक ही समझने लगे थे. यानि एक समय देश के पहले आम चुनाव (1951-52) में कांग्रेस के सामने देश के मुख्य विपक्षी दल बने वामपंथी अगले ढाई दशकों में ही उनके शरण में आ गये. और राजनीति में स्वतंत्र अस्तित्वहीन विचारधारा की मृत्यु तो नियति का अवश्यंभावी सत्य है.
1978 में एक भाकपा नेता ने पार्टी की ग्यारहवीं कांग्रेस में स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की स्वतंत्र भावमूर्ति धूमिल हो गयी थी और लोग उसे तथा तत्कालीन शासक को एक ही समझने लगे थे. यानि एक समय देश के पहले आम चुनाव (1951-52) में कांग्रेस के सामने देश के मुख्य विपक्षी दल बने वामपंथी अगले ढाई दशकों में ही उनके शरण में आ गये. और राजनीति में स्वतंत्र अस्तित्वहीन विचारधारा की मृत्यु तो नियति का अवश्यंभावी सत्य है. इस वैचारिक हठधर्मिता की स्थिति को दूसरे रूप में कहें तो भारत में वामपंथ के मानस संतानों की मानसिकता यह है कि वे दो सौ सालों पुराने तत्कालीन यूरोप की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित वैचारिकी को आज के आधुनिक भारतीय परिस्थितियों पर लागू करना चाहते हैं. ऐसे में उनकी स्थिति वर्तमान इस्लामिक कट्टरपंथियों से बिलकुल भी अलग नहीं है जो आज डेढ़ हजार से भी अधिक पुराने पंथीय विचारों को तत्कालीन अरबी राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों से उभरे थे, वर्तमान 21वीं सदी में जीना चाहते हैं. और इन दोनों के लिए सबसे हास्यास्पद स्थित यह है कि इनके सैद्धांतिक विचारों की जन्मभूमि आज स्वयं अपनी पुरातन मान्यताओं को अस्वीकृत करते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर है. यूरोप समवाय एवं समानता पर आधारित आधुनिक समाज बना रहा है और भारत के वामपंथी अभी भी वर्ग-संघर्ष के प्रणेता बने रहना चाहते हैं वैसे ही जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी बुरखा को सार्वजानिक स्वीकृति दिलाने पर आमादा है और उधर सऊदी अरब ऐसी इस्लामिक संस्कृति को गैर-राष्ट्रीय मानते हुए परे हटा रहा है बल्कि ब्यूटी कांस्टेंट में अपने प्रतिनिधि भेज रहा है. अब इसे जड़ता की पराकाष्ठा ना समझें तो. और क्या कहें.
वामपंथ आज स्वयं इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसके स्वयं ऐतिहासिक होने का संकट पैदा हो गया. हो सकता है कि लोकतंत्र के सैद्धांतिक संघर्ष में आलोचक वर्ग वामपंथ या किसी भी अन्य वैचारिक आंदोलन के पराभूत होने का जश्न मना सकता है लेकिन ये समझना आवश्यक है कि एक विचारधारा का आंदोलन अपने पीछे एक समृद्ध अतीत समेटे होता जिसमें वह आशाएँ, वे उम्मीद होती हैं जो उसके अनुयायियों ने संजो रखी होती है. इससे वे दर्द, वे आँसू होते हैं जो इस संघर्ष में उपजे होते. वे सीख होती हैं जो जम्हुरियत के अनुभव को व्यापक आकार देती हैं. इन सबसे बढ़कर एक विचारधारा लोकतान्त्रिक विकल्प का प्रमुख स्तम्भ बने रहना जरुरी है क्योंकि जनतन्त्र में वैचारिक विकल्पों का सिमटना उसके भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं होता है. इस चेतावनी, इस आशंका को सबसे पहले वामपंथी नेतृत्व को समझने एवं स्वीकारने की जरुरत है.
