 किसी भी राष्ट्र के जीवन में कठिन दौर तब आता है ज़ब उसकी राजनीति दिशाहीन और राष्ट्रीय हितों के ऊपर सत्ता स्वार्थ को तरजीह देने लगे. भारत में जातिगत जनगणना ने राजनीति के इसी कुत्सित अवस्था का नग्न यथार्थ प्रदर्शित किया. बिहार में हुई जातिगत जनगणना ने विकृतियों के एक ऐसे पिटारे को खोल दिया है जिसमें एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए समस्या का अंबार है या यूँ कहें कि इसने राष्ट्रीय एकता को एक अनजाने और डरावने भविष्य की ओर धकेल दिया है. इसकी बानगी दिखी ज़ब एक तरफ एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का विमर्श जाति आधारित जनगणना के परिणाम एवं प्रभाव की विवेचना में व्यस्त था तब इस जातिवाद के परोक्ष प्रभाव के रूप उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की माँग हुई.
किसी भी राष्ट्र के जीवन में कठिन दौर तब आता है ज़ब उसकी राजनीति दिशाहीन और राष्ट्रीय हितों के ऊपर सत्ता स्वार्थ को तरजीह देने लगे. भारत में जातिगत जनगणना ने राजनीति के इसी कुत्सित अवस्था का नग्न यथार्थ प्रदर्शित किया. बिहार में हुई जातिगत जनगणना ने विकृतियों के एक ऐसे पिटारे को खोल दिया है जिसमें एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए समस्या का अंबार है या यूँ कहें कि इसने राष्ट्रीय एकता को एक अनजाने और डरावने भविष्य की ओर धकेल दिया है. इसकी बानगी दिखी ज़ब एक तरफ एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का विमर्श जाति आधारित जनगणना के परिणाम एवं प्रभाव की विवेचना में व्यस्त था तब इस जातिवाद के परोक्ष प्रभाव के रूप उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की माँग हुई.केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनडीए गठबंधन के सहयोगी सुभासपा प्रमुख ने पूर्वांचल के रूप में पृथक राज्यों की माँग की. प्रतीत होता है कि स्वयं को विकास के सशक्त अग्रदूत मानने वाले सत्ताधारी एनडीए गठबंधन सरकार के पास या तो जिताऊ मुद्दों की कमी है या फिर उसकी सुविचारित रणनीति का परिणाम. इन माँगों में सत्ता या सरकार की स्वीकृति कितनी है, यह अलग बहस का विषय है परन्तु राजनीति की यह दिशा नकारात्मकता की प्रसारक है. पहले से ही विघटनवादी शक्तियों की उपद्रव से जूझ रहे राष्ट्र में जातीय संकीर्णता को बढ़ावा देने का प्रयास समझ से परे है.
वैसे ये छोटे राज्यों की माँग अनायास नहीं है. यह उस सुविचारित लोकतंत्र विरोधी षड़यंत्र का हिस्सा है जहाँ जातियों की गोलबंदी से सत्ता का साम्राज्य खड़ा करने का स्वप्न देखा जा रहा है. कैसे, समझिये. पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल यहाँ कुछ जाति विशेष की सघनता है तो कुछ जातियों की प्रभाविता इन मांगों के आधार में यही केंद्र बिन्दु है.
 बात सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की ही कर लेते हैं जो स्वयं को राजभर जाति का एकमात्र स्वयंभु नेता मानते हैं. पूर्वांचल में राजभर जाति की आबादी लगभग 12 से 22 प्रतिशत होने का अनुमान है. आकलन बताते हैं कि पूर्वांचल की घोसी बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी जैसी दो दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट पचास हजार से ढ़ाई लाख तक हैं जो हार-जीत के निर्णयन के लिए अत्यावश्यक हैं. इस संख्या बल को दिशा की अपनी क्षमता के कारण ही दो दशकों से भी अधिक समय से जातिवाद में सने ओमप्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाये हुए हैं.
बात सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की ही कर लेते हैं जो स्वयं को राजभर जाति का एकमात्र स्वयंभु नेता मानते हैं. पूर्वांचल में राजभर जाति की आबादी लगभग 12 से 22 प्रतिशत होने का अनुमान है. आकलन बताते हैं कि पूर्वांचल की घोसी बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी जैसी दो दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट पचास हजार से ढ़ाई लाख तक हैं जो हार-जीत के निर्णयन के लिए अत्यावश्यक हैं. इस संख्या बल को दिशा की अपनी क्षमता के कारण ही दो दशकों से भी अधिक समय से जातिवाद में सने ओमप्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाये हुए हैं.कुछ ऐसा ही मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य की माँग के उद्घोषक संजीव बालियान का भी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आबादी करीब 17 फीसदी है. बालियान जैसे नेता जानते है कि इस जातीय आबादी के सहारे कितनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तुष्ट किया जा सकता है. अतः ऐसे ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह और सर छोटूराम के लिए भारत रत्न की माँग नहीं की. ये सारी बयानबाजी जातिगत गोलबंदी और साथ ही अपना अस्तित्व बनाये का प्रयास ही थी.
असल में 2019 के आम चुनाव में न्यूनतम मतों के अंतर से सीट बचाने में सफल हुए बालियान अपने जातिगत आधार जाट जाति में अपने प्रभाव के विस्तार में लगे हैं ताकि कुर्सी बची रहे. कुछ ऐसी ही स्थिति ओमप्रकाश राजभर की भी है. घोसी उपचुनाव में भाजपा के दूत बनकर किला बचाने गये राजभर अपमानजनक चुनावी पराजय को पचाने की जुगत में हैं. अपने बिदकते जातिगत आधार को जोड़े रखने के लिए वे निरंतर जुगत में लगे हैं. अतः इन नेताओं के अलग राज्यों की माँग को इसी राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए.
जातिगत राजनीति करने वालों का भारतीय राजनीति में आधार ही उनका स्वजाति के संख्याबल के आधार पर स्थापित दबाव है. देश के विभिन्न राज्यों में प्रभावी क्षेत्रीय दलों का तो 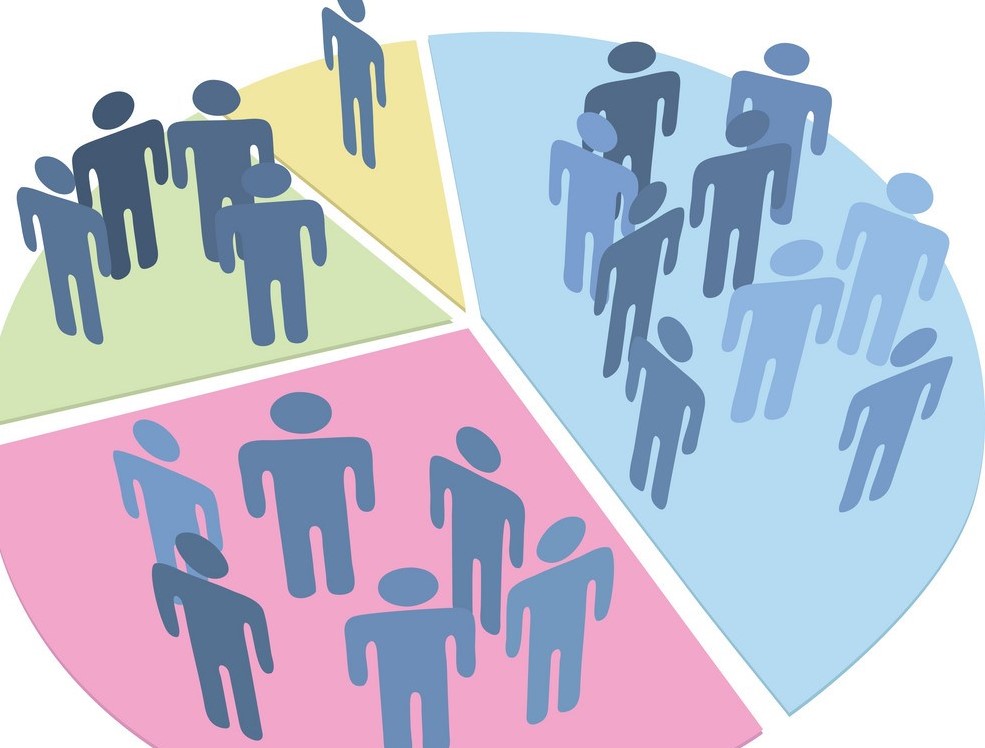 आधार ही जातिवाद है साथ ही भाजपा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का इस आधार पर समर्थन तलाशना भी कोई ढका-छुपा मामला नहीं है. लेकिन समस्या यह है कि जातीय एवं धार्मिक गोलबंदी के सहारे सत्ता की राजनीति अब दिनोदिन विध्वँसक रूप लेती जा रही है. कुमार विश्वास ने कुछ समय पूर्व अरविन्द केजरीवाल पर खालिस्तानियों के समर्थन एवं पंजाब के विघटन के पश्चात् एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने का आरोप लगाया था. अब इसमें कितनी सत्यता ये तो वही जाने किन्तु यह एक राजनीतिक दुरभीसंधियों का एक विकृत उदाहरण है.
आधार ही जातिवाद है साथ ही भाजपा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का इस आधार पर समर्थन तलाशना भी कोई ढका-छुपा मामला नहीं है. लेकिन समस्या यह है कि जातीय एवं धार्मिक गोलबंदी के सहारे सत्ता की राजनीति अब दिनोदिन विध्वँसक रूप लेती जा रही है. कुमार विश्वास ने कुछ समय पूर्व अरविन्द केजरीवाल पर खालिस्तानियों के समर्थन एवं पंजाब के विघटन के पश्चात् एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने का आरोप लगाया था. अब इसमें कितनी सत्यता ये तो वही जाने किन्तु यह एक राजनीतिक दुरभीसंधियों का एक विकृत उदाहरण है.
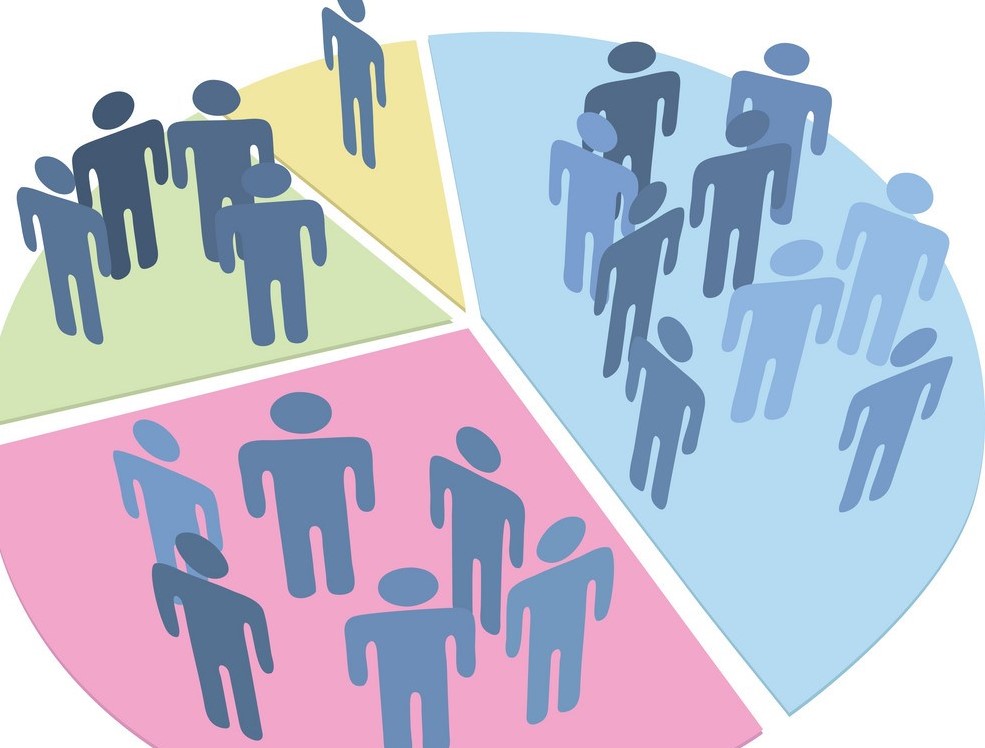 आधार ही जातिवाद है साथ ही भाजपा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का इस आधार पर समर्थन तलाशना भी कोई ढका-छुपा मामला नहीं है. लेकिन समस्या यह है कि जातीय एवं धार्मिक गोलबंदी के सहारे सत्ता की राजनीति अब दिनोदिन विध्वँसक रूप लेती जा रही है. कुमार विश्वास ने कुछ समय पूर्व अरविन्द केजरीवाल पर खालिस्तानियों के समर्थन एवं पंजाब के विघटन के पश्चात् एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने का आरोप लगाया था. अब इसमें कितनी सत्यता ये तो वही जाने किन्तु यह एक राजनीतिक दुरभीसंधियों का एक विकृत उदाहरण है.
आधार ही जातिवाद है साथ ही भाजपा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का इस आधार पर समर्थन तलाशना भी कोई ढका-छुपा मामला नहीं है. लेकिन समस्या यह है कि जातीय एवं धार्मिक गोलबंदी के सहारे सत्ता की राजनीति अब दिनोदिन विध्वँसक रूप लेती जा रही है. कुमार विश्वास ने कुछ समय पूर्व अरविन्द केजरीवाल पर खालिस्तानियों के समर्थन एवं पंजाब के विघटन के पश्चात् एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने का आरोप लगाया था. अब इसमें कितनी सत्यता ये तो वही जाने किन्तु यह एक राजनीतिक दुरभीसंधियों का एक विकृत उदाहरण है. वैसे भी आजकल देश में लोगों की जातिगत भावनाएं इतनी विध्वंसक हो चुकी है कि राष्ट्रीय नायकों तक की जाति तलाश की जा रही है. उदाहरणस्वरुप अब यह पता करने की लड़ाई लड़ रहे चल रही है कि महाराज सुहेलदेव राजभर जाति के थे या कि खटीक-पासी. ऐसे में भावनात्मक मुद्दों के आधार पर जातिगत गोलबंदी कोई कठिन कार्य नहीं है. लेकिन जनता को समझना होगा कि ये ढोंगी राजनीतिज्ञ छोटे राज्यों की माँग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हें समान विकास और सहभागी लोकतंत्र की चिंता नहीं है बल्कि इनकी माँग का आधार सत्ता सुख की चाह है, भले की इसके लिए संकीर्ण मुद्दों के सहारे समाज को भड़काकर सबकुछ जलाना पड़े.
यह इतिहास का यथार्थ है. भारत आजादी के शैशवकाल में ज़ब खुद को जोड़ने में लगा था तब भाषाई आधार पर प्रांतीय विभाजन की माँग ने विद्रुप विघटनकारी हालात पैदा कर दिये थे. तब इस समस्या के निराकरण हेतु गठित जेवीपी कमेटी का तर्क था कि, ‘भाषा महज जोड़ने वाली ही नहीं बल्कि एक-दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है. अभी प्राथमिक ध्यान देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक विकास पर होना चाहिए, इसलिए हरेक अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृतियों को मजबूती से हतोत्साहित किया जाना चाहिए.’
यह भविष्य के लिए एक संदेश था. अतः जब राष्ट्रीय स्तर का विमर्श भाषा को अलग राज्य के गठन का आधार मानने कों स्वीकृत नहीं कर रहा था फिर आज जाति जैसी कहीं संकीर्ण संस्था को कैसे स्वीकार किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में संकीर्ण माँगों की स्वीकृति के पश्चात् उसकी आधारिक भावना का शमन हो जाता है बल्कि यह एक नकारात्मक भावनाओं पर आधारित श्रृंखला का रूप धारण करती है जो अगले हर बार अधिक विकृत रूप में उपस्थित होता है. जैसा कि हीगल का द्वन्दवाद ‘वाद-प्रतिवाद एवं संवाद’ एक ऐसी ही निरंतर गतिशील प्रक्रिया की व्याख्या करता है.
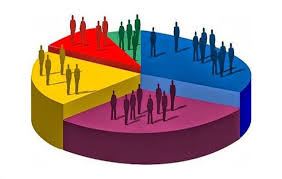 हालांकि भारत में इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. राष्ट्र के रूप में भारत एक ठोस ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है और यही वज़ह है कि यह अब भी एक रचना प्रक्रिया से गुजर रहा है. जिसमें भारतीय होने की भावना एवं प्रबल आधार है. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ‘भारत की एकता भावनाओं की एकता है.’ किन्तु इस भावना के नीचे एक आतंरिक संघर्ष सदैव पलता रहा है. यह एक सामान्य सा विमर्श है कि आर्थिक संसाधनों में अधिक की हिस्सेदारी, शैक्षणिक एवं रोजगार के अवसर, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा इब जातिवाद जैसे मुद्दे राष्ट्रीय-सामाजिक जीवन में संघर्षों का आधार ही नहीं बनते हैं बल्कि उन्हें भड़काते भी है. भारत के पिछले एक सदी के इतिहास के सिंहावलोकन से इस तर्क की सहज़ पुष्टि हो सकती है
हालांकि भारत में इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. राष्ट्र के रूप में भारत एक ठोस ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है और यही वज़ह है कि यह अब भी एक रचना प्रक्रिया से गुजर रहा है. जिसमें भारतीय होने की भावना एवं प्रबल आधार है. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ‘भारत की एकता भावनाओं की एकता है.’ किन्तु इस भावना के नीचे एक आतंरिक संघर्ष सदैव पलता रहा है. यह एक सामान्य सा विमर्श है कि आर्थिक संसाधनों में अधिक की हिस्सेदारी, शैक्षणिक एवं रोजगार के अवसर, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा इब जातिवाद जैसे मुद्दे राष्ट्रीय-सामाजिक जीवन में संघर्षों का आधार ही नहीं बनते हैं बल्कि उन्हें भड़काते भी है. भारत के पिछले एक सदी के इतिहास के सिंहावलोकन से इस तर्क की सहज़ पुष्टि हो सकती है स्वतंत्र भारत में इन सभी मसलों पर आधारित विभिन्नता एक भेदभाव के निराकरण का जिस तरह प्रयास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं या यूँ कहे की विकास के विस्तार और उसकी सर्वसुलभता लोकतान्त्रिक उम्मीदों के अनुकूल नहीं रहीं. इसकी सबसे बड़ी वज़ह राजनीतिक काहिलियत और ठोस निर्णयन की क्षमता का अभाव था. परिणाम ये हुआ कि उपरोक्त आधारों, चाहे वह भाषा, क्षेत्र या जाति हो, से सम्बंधित समुदाय के अंदर अपने साथ के भेदभाव की भावना से प्रश्रयित क्रोध पलता रहा जिसकी शान्त, उग्र ही नहीं बल्कि कई दफ़े विध्वँसक अभिव्यक्ति हुईं. इसमें भी जाति जो सबसे कठोर या संकीर्ण संस्था रही, के आधार पर भेदभाव झेलने वालों ने ब्राह्मणवाद को अपना सर्वप्रमुख सैद्धांतिक शत्रु मान लिया और यही उनके विरोध का केन्द्र बन गया. इसके प्रवर्तक के रूप में तथाकथित सवर्ण जातियों के लिए तथाकथित पिछड़ी और दलित जातियों में कटुता स्थायी रूप लेती गईं जिसमें बीतते समय के साथ तर्कहीनता घटती रही और अंधविरोध बढ़ता रहा और यही आज कटुता आज देश को एक ख़तरनाक मोड़ तक घसीट लाई है जहाँ वह राष्ट्रीय जीवन के ध्वँस पर आमादा है.
असल में ब्राह्मणवाद-मनुवाद के विरोध के नाम पर जातिवाद के जिस जिन्न को बोतल से निकाला गया है उसकी अभिशप्त छाया लोकतंत्र को ग्रसने लगी है और इसके व्यापक दुष्परिणामों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए. लेकिन उससे अधिक आवश्यक है जातिवाद के सहारे सामाजिक विघटन को उद्यत इन अवसरवादियों के घातक मनोभावों को समझना. इन्हें अपनी या किसी जाति के विकास से कोई सरोकार नहीं बल्कि इनका ध्येय सत्ता सुख-भोग है और उसके लिए चाहे इन्हें सामाजिक एकता या राष्ट्रीय हितों को भी दाव पर लगाना पड़े. जैसा कि प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक आलोचक, अभिनेता और लेखक जॉर्ज कार्लिन कहते हैं, ‘एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है.’ तो जनता इन्हें देखें, समझें ताकि इनके स्वार्थ के प्रतिकार के साथ ही राष्ट्रीय भविष्य को विध्वँस की राह पर जाने से रोक सके.
