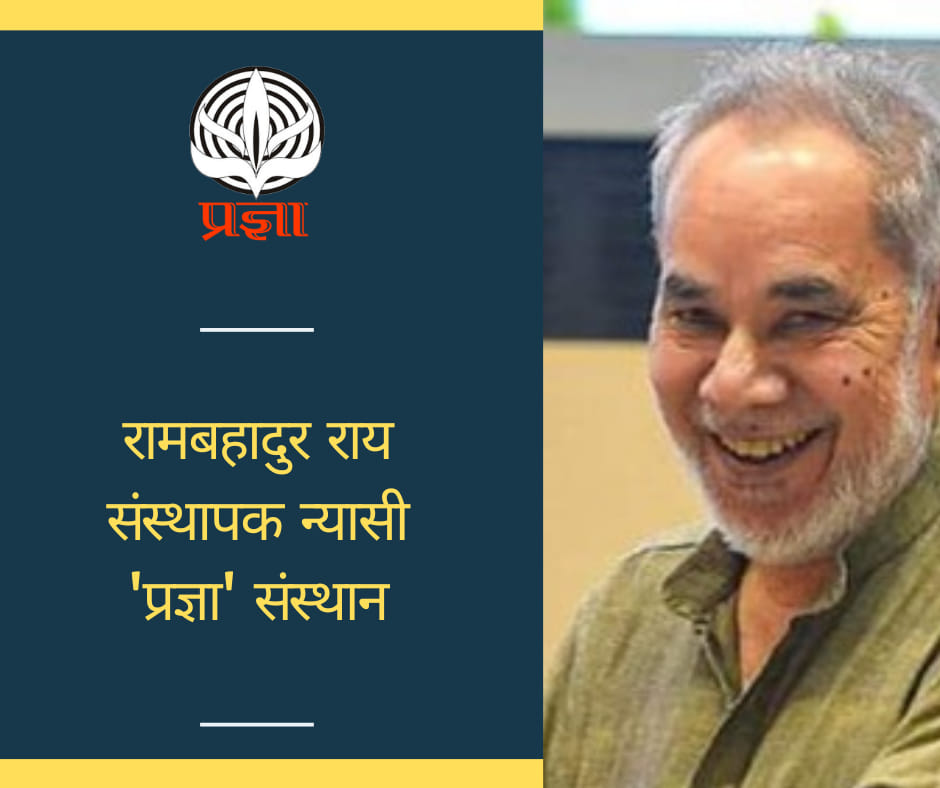
विपक्षी एकता कोई नई बात नहीं है। पहले विपक्षी एकता का आधार वैचारिक होता था अब यह स्वार्थ आधारित हो गया है। लेकिन यह विडंबना ही है कि इन दिनों जो लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं वे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं।
अपनी पार्टी जो-जो नहीं संभाल पा रहे हैं वे विपक्ष को एकजुट करने का झंडा उठाए अवारा बादलों की भांति आकाश में विचरण कर रहे हैं। विपक्षी एकता की यह विडंबना कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। आजादी के बाद एक दौर था, वैचारिक राजनीति का। उस दौर में दलों का एका विचार आधारित होता था। इसके अपवाद भी हैं। एक अपवाद प्रसोपा का गठन भी था। जिसके दिग्गज आचार्य जे.बी. कृपलानी और जयप्रकाश नारायण थे। वह वैचारिक एकता भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि समाजवादी होने का रंग-बिरंगा अहंकार इतना बड़ा था कि थोड़े ही दिनों बाद वह एकता बिखर गई। जिस तरह मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि बिखरे बादल कभी बरसते नहीं और उन्हें हवा उड़ा ले जाती है, उनका पता भी नहीं चलता कि आकाश में कोई अस्तित्व था। इस उपमा को प्रसोपा पर सटीक बैठाया जा सकता है। क्या किसी को याद है कि प्रसोपा नाम की एक पार्टी थी? क्या यह भी याद है कि उसमें राजनीति के त्यागी, स्वाधीनता संग्राम के तपस्वी और सचमुच जिसे विद्वता कहते हैं उसके धनी अनेक नाम थे।
उनके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो राजनीति के आकाश में आज भी चमकता सितारा है। वे आचार्य नरेंद्र देव हैं। जिनके बारे में अक्सर चंद्रशेखर कहा करते थे कि सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव ही हैं जिनकी ऊंचाई को छू लेने का कभी मैं सपना भी नहीं देखता। यह कथन उस व्यक्ति का है जो पूर्व प्रधानमंत्री था। जो किसी से भी दबकर बात नहीं करता था। सबसे बराबरी पर बात करता था। दूसरे भी उनका लोहा मानते थे। लेकिन जैसा हाल प्रसोपा का हुआ, वैसा ही जनता पार्टी का हुआ। जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे।
 इमरजेंसी का असहनीय ताप इतना तीखा था कि राजनीति के हर तरह के जीव-जंतु एक राजनीतिक दल रूपी काल्पनिक वृक्ष के तले आ गए। कैसे बनी जनता पार्टी? इसे जो आज जानेगा वह विपक्षी एकता के उस सूत्र को आसानी से अपना भाष्य करके समझ लेगा। उसकी समझ सच्ची होगी, कच्ची नहीं होगी। वह आजाद भारत के चंद साल पहले के राजनीतिक इतिहास की किताब से सही पाठ अपने लिए खोज लेगा। यहां आशय उस नागरिक से है जो संविधान में संप्रभु है। प्रभुता उसमें निहित है। वही अपने स्तर पर इसका निर्धारण करता है कि कौन है जो देश को चला सकेगा। उसकी क्षमता को फलने-फूलने का मौका देगा। देश को भ्रम और भटकन से निकाल सकेगा। वही समय का सच निर्धारित करता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 18 जनवरी, 1977 को इंदिरा गांधी ने यह सोचकर लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी कि उन्हें लोग जिताएंगे। इस तरह उनकी तानाशाही पर जनता की मुहर लग जाएगी और संजय गांधी के कारनामों को लोग भुला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको बताने की यहां जरूरत नहीं है। यहां तो यह जानने की जरूरत है कि विपक्ष को एक करने की लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कोशिश उन दिनों कैसे विफल हो गई जब देश में इमरजेंसी का घोर अंधियारा था। उस कालखंड में जेपी की दृष्टि में लोकतांत्रिक विपक्ष की एकता से अंधियारा के छटने का संदेश जन-जन में जाता। उस कोशिश पर सबसे प्रामाणिक जानकारी शांतिभूषण की आत्मकथा में है। वे उस प्रयास में जेपी के एक सहयोगी थे। उसका सार अगर एक-दो वाक्यों में कहना हो तो यह है कि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एस.एम. जोशी सहित उन दलों के प्रतिनिधि नेताओं का अहंकार टकराता रहता था। जिसके कारण विपक्ष की एकता दूर की कौड़ी होती थी जबकि जेपी चाहते थे कि इमरजेंसी का लोकतांत्रिक जवाब देने के लिए लोकदल, सोपा (सोशलिस्ट पार्टी), कांग्रेस (संगठन) और जनसंघ को मिलाकर एक राजनीतिक दल बन जाए।
इमरजेंसी का असहनीय ताप इतना तीखा था कि राजनीति के हर तरह के जीव-जंतु एक राजनीतिक दल रूपी काल्पनिक वृक्ष के तले आ गए। कैसे बनी जनता पार्टी? इसे जो आज जानेगा वह विपक्षी एकता के उस सूत्र को आसानी से अपना भाष्य करके समझ लेगा। उसकी समझ सच्ची होगी, कच्ची नहीं होगी। वह आजाद भारत के चंद साल पहले के राजनीतिक इतिहास की किताब से सही पाठ अपने लिए खोज लेगा। यहां आशय उस नागरिक से है जो संविधान में संप्रभु है। प्रभुता उसमें निहित है। वही अपने स्तर पर इसका निर्धारण करता है कि कौन है जो देश को चला सकेगा। उसकी क्षमता को फलने-फूलने का मौका देगा। देश को भ्रम और भटकन से निकाल सकेगा। वही समय का सच निर्धारित करता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 18 जनवरी, 1977 को इंदिरा गांधी ने यह सोचकर लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी कि उन्हें लोग जिताएंगे। इस तरह उनकी तानाशाही पर जनता की मुहर लग जाएगी और संजय गांधी के कारनामों को लोग भुला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको बताने की यहां जरूरत नहीं है। यहां तो यह जानने की जरूरत है कि विपक्ष को एक करने की लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कोशिश उन दिनों कैसे विफल हो गई जब देश में इमरजेंसी का घोर अंधियारा था। उस कालखंड में जेपी की दृष्टि में लोकतांत्रिक विपक्ष की एकता से अंधियारा के छटने का संदेश जन-जन में जाता। उस कोशिश पर सबसे प्रामाणिक जानकारी शांतिभूषण की आत्मकथा में है। वे उस प्रयास में जेपी के एक सहयोगी थे। उसका सार अगर एक-दो वाक्यों में कहना हो तो यह है कि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एस.एम. जोशी सहित उन दलों के प्रतिनिधि नेताओं का अहंकार टकराता रहता था। जिसके कारण विपक्ष की एकता दूर की कौड़ी होती थी जबकि जेपी चाहते थे कि इमरजेंसी का लोकतांत्रिक जवाब देने के लिए लोकदल, सोपा (सोशलिस्ट पार्टी), कांग्रेस (संगठन) और जनसंघ को मिलाकर एक राजनीतिक दल बन जाए।जेपी खतरे को सही भांप रहे थे। उनकी भूमिका उस समय वैसी ही थी, जैसी आजादी के समय महात्मा गांधी की थी। जेपी की नेक सलाह अहंकारी राजनीतिक नेताओं के गले नहीं उतरी। हां, जब चुनावों की घोषणा हो गई तो अपना स्वार्थ देखकर वे एक दल बनाने के लिए बामुश्किल तैयार हुए। चुनाव की घोषणा के अगले दिन ही जनता पार्टी का गठन हो सका। लेकिन जनता पार्टी क्या लोगों की आशा-आकांक्षा को पूरा कर सकी? यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि वह ऐसी ज्ञात दुर्घटना है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जिस राजनारायण ने इंदिरा गांधी को मुकदमे में हराया। जिसके कारण इमरजेंसी लगी, उसी राजनारायण ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर संजय गांधी की गोद में बैठना स्वीकार किया।
जनता पार्टी की सरकार छिन्न-भिन्न हो गई। यह सब जानते हैं। जो सरकार में थे और जिन पर पार्टी चलाने का जिम्मा था, वे विपरीत दिशाओं में चलने-सोचने के अभ्यस्त थे। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था। प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बन सकता है। लोगों ने उसी महिला को पुन: सत्ता सौंपी, जिन्हें हटा दिया था। जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में आईं कि वे नेता जो अपनी पार्टी नहीं चला सके और जनता ने जिन्हें हाशिए पर डाल दिया था वे विपक्षी एकता के लिए जगह-जगह जमावड़ा करने लगे। अखबार उन्हें सुर्खियां देते थे। अंग्रेजी में ‘अपोजिशन कान्क्लेव’ का नामकरण उन दिनों खूब चर्चित था। कुछ लोग उम्मीदें भी करते थे क्योंकि उस जमावड़े में जो आते थे वे बड़े नाम थे। ऐसे अनेक जमावड़े हुए। उस जमावड़े के कुछ चर्चित नाम आज भी भारत की राजनीति में हैं और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे, फारुक अब्दुल्ला, शरद पवार, परकाश सिंह बादल। जो नहीं हैं उनका नाम लेना उचित नहीं होगा।
 उस जमावड़े से कुछ निकला नहीं। नेताओं की दौड़-भाग जारी रही। वैसे ही जैसे बांझ विपक्षी एकता। अस्तित्व का संकट हो तो एकता भले ही थोड़े समय की हो, पर हो जाती है। आज क्या अस्तित्व का संकट है? इस संकट के दो रूप हैं। अगर नागरिक का अस्तित्व संकट में पड़ता है तो उसकी राजनीतिक गत्यात्मकता इतनी प्रबल होती है कि वह अहंकारी नेताओं को भी एक मंच पर आने और स्वार्थ के ही कारण सही पर बने रहने के लिए मजबूर कर देती है। संकट का यह रूप अब तक विपक्षी एकता का कारक रहा है। चाहे वह 1977 हो या 1989। संकट का जो दूसरा रूप है वह इस समय ज्यादा प्रासंगिक है और वही रूप वास्तव में समझने जैसा है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल रहा है। वह अब एक परिवार का बंधक है।
उस जमावड़े से कुछ निकला नहीं। नेताओं की दौड़-भाग जारी रही। वैसे ही जैसे बांझ विपक्षी एकता। अस्तित्व का संकट हो तो एकता भले ही थोड़े समय की हो, पर हो जाती है। आज क्या अस्तित्व का संकट है? इस संकट के दो रूप हैं। अगर नागरिक का अस्तित्व संकट में पड़ता है तो उसकी राजनीतिक गत्यात्मकता इतनी प्रबल होती है कि वह अहंकारी नेताओं को भी एक मंच पर आने और स्वार्थ के ही कारण सही पर बने रहने के लिए मजबूर कर देती है। संकट का यह रूप अब तक विपक्षी एकता का कारक रहा है। चाहे वह 1977 हो या 1989। संकट का जो दूसरा रूप है वह इस समय ज्यादा प्रासंगिक है और वही रूप वास्तव में समझने जैसा है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल रहा है। वह अब एक परिवार का बंधक है। कांग्रेस में बंधक राजनीति से मुक्ति की इच्छा है। उसी का दृश्य इस समय कांग्रेस की हलचलों में देखा जा सकता है।
कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी हैं। जो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। उनके बारे में पार्टी और समाज में एक सी धारणा है। वह यह कि वे अधिकार तो चाहते हैं और वह भी पूर्ण अधिकार, लेकिन जिम्मेदारी के लिए उन्हें दूसरे उस कंधे की तलाश है जिसे जरूरत पड़ने पर बलि का बकरा बनाया जा सके। ऐसा कोई उनको खोजे नहीं मिल रहा है। जिसे वे खोज रहे हैं वह अपनी शर्तें उनके सामने भले कहे या नहीं, लेकिन उसके समर्थक ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। आखिर यही तो वजह है कि अशोक गहलोत के समर्थक इतने उग्र हुए कि सोनिया गांधी के दूतों को अपमानित होकर लौटना पड़ा। जरा याद करें, आठवें दशक के प्रारंभ में एक दिन सीताराम केसरी भोपाल गए। विधान सभा के चुनाव हो गए थे। कांग्रेस को बहुमत मिला था। प्रश्न था कि मुख्यमंत्री कौन हो? विधायक दल की बैठक हुई। सीताराम केसरी बोले, आप सबकी ओर से अर्जुन सिंह को विधायक दल का नेता चुने जाने पर मैं बधाई देता हूं। यह कहकर उन्होंने एक माला अर्जुन सिंह के गले में डाल दी। विधायकों ने समझा कि इंदिरा गांधी का यही निर्देश है। उनके मन में क्या था, यह परमात्मा जानते हैं।
उस इंदिरा गांधी की उत्तराधिकारी हैं, सोनिया गांधी। जिनके दूत अपमानित होकर लौट रहे हैं। लेकिन जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का झंडा प्रतिक्रिया में उठाकर चलने के लिए पहला कदम उठाया है, उस खिलाड़ी को खेल के नियम याद नहीं हैं। अगर होते तो वे भ्रष्टाचार के अपराध में सजा पाए ओम प्रकाश चौटाला की सदारत में मंच पर नहीं जाते। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह किसी ऐसे मंच पर गए जहां भ्रष्टाचार के आरोपी नेता होते थे? इसे क्या कहेंगे? यही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हद तो तब हो गई जब सोनिया गांधी से मिलने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पहुंचे। विपक्षी एकता का प्रयास जिन-जिन नेताओं ने जब-जब किया और वे जब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो क्या वे इस अनाड़ीपन को सहन करते! क्या चुप रहते? वे यह सवाल पूछते कि जिस सोनिया गांधी से कांग्रेस नहीं संभल रही है उन्हीं से विपक्ष की एकता का वरदान मांगने जाना क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ पर बड़ा सवाल नहीं है?
