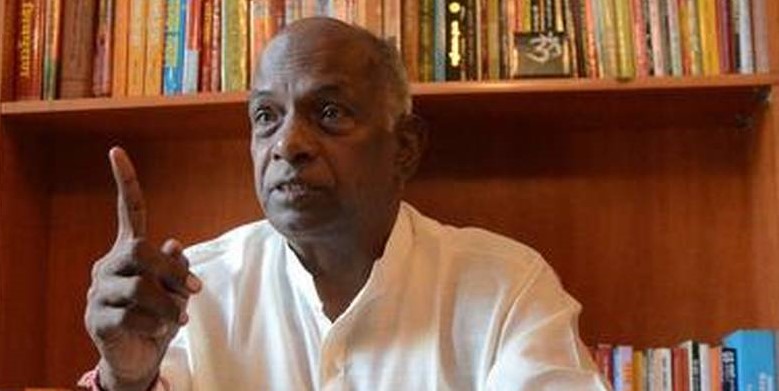 हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र केवल भौतिक साधनों से उन्नत नहीं हुआ करते। यदि ऐसा होता तो जापान कभी एक उन्नत राष्ट्र नहीं बन पाता। यह ऐसा देश है जहां कहीं ठंड होती है तो कहीं भयानक पाला पड़ता है। खेती खुद के खाने लायक भी नहीं है। आए दिन भूकंप आते हैं सो अलग। कुछ लोगों ने कहा कि तेल के कारण खाड़ी देशों का विकास हो गया। लेकिन, वे लोग भूल गए कि वेनेजुएला में भी तो तेल है, वह क्यों आगे नहीं बढ़ा? यदि थाईलैंड, वियतनाम बढ़ गये तो उसी जलवायु का फिलीपींस भी है, वह क्यों नहीं बढ़ा? वास्तव में देश केवल साधन और तकनीक से नहीं बढ़ते। देश केवल आयात-निर्यात की मात्रा के आधार पर आगे बढ़ते। देश उनकी अपनी तासीर से बढ़ते हैं। उनके अपने लोगों के जज्बे लगन से बढ़ते हैं। देश उन्नति करते हैं अपने लोगों के जीवन मूल्यों एवं अपनी सामाजिक पूंजी के बल पर।
हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र केवल भौतिक साधनों से उन्नत नहीं हुआ करते। यदि ऐसा होता तो जापान कभी एक उन्नत राष्ट्र नहीं बन पाता। यह ऐसा देश है जहां कहीं ठंड होती है तो कहीं भयानक पाला पड़ता है। खेती खुद के खाने लायक भी नहीं है। आए दिन भूकंप आते हैं सो अलग। कुछ लोगों ने कहा कि तेल के कारण खाड़ी देशों का विकास हो गया। लेकिन, वे लोग भूल गए कि वेनेजुएला में भी तो तेल है, वह क्यों आगे नहीं बढ़ा? यदि थाईलैंड, वियतनाम बढ़ गये तो उसी जलवायु का फिलीपींस भी है, वह क्यों नहीं बढ़ा? वास्तव में देश केवल साधन और तकनीक से नहीं बढ़ते। देश केवल आयात-निर्यात की मात्रा के आधार पर आगे बढ़ते। देश उनकी अपनी तासीर से बढ़ते हैं। उनके अपने लोगों के जज्बे लगन से बढ़ते हैं। देश उन्नति करते हैं अपने लोगों के जीवन मूल्यों एवं अपनी सामाजिक पूंजी के बल पर।
दुनिया के प्रत्येक हिस्से में समाज संचालन की विधा अलग-अलग होती है। यूरोप का समाज राजसत्ता द्वारा नियंत्रित है जबकि भारतीय समाज में राजसत्ता की भूमिका निर्णायक नहीं है। यहां समाज आज भी धर्मसत्ता, समाजसत्ता, अर्थसत्ता और राजसत्ता के सम्मिलित प्रयासों से संचालित होता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी घुसपैठ की है, फिर भी भारतीय संदर्भ में समाज आज भी मुख्यतः अपने बनाए मूल्यों एवं परंपराओं के बल पर चल रहा है। राज्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था क पूरक मात्र है। इसका उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। हमें अपने और पड़ोसियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए पुलिस वालों की जरूरत कम होती है। भारत में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पुलिस कभी नहीं गई। अमेरिका में 10 हजार नागरिकों पर 130 पुलिस वाले हैं। जबकि भारत में 10 हजार लोगों पर पुलिस का केवल एक आदमी है। फिर भी अमेरिका की तुलना में भारत में अपराध कम हैं। ऐसा इसलिए संभव है, क्योंकि हमारे यहां लोग बड़ों का लिहाज करते हैं और आंखों की शरम बचा के चलते हैं। लोग यदि अपराध नहीं करते तो इसके पीछे पुलिस का डर उतना काम नहीं करता जितना अपनी तथा अपने परिवार की इज्जत की चिंता और परलोक का डर काम करता है।
भारतीय समाज के संचालन में हमेशा से एक विश्व दृष्टि रही है। मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं है। प्रकृति केवल उसके उपभोग के लिए रची हुई नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पवित्र है और पर्यावरण की रक्षा सबका कर्तव्य है। ये बातें भारत के आम आदमी में कई सदियों से मान्यता प्राप्त हैं। बिश्नोई जाति के लोगों की वृक्षों को बचाने की परंपरा इसी विश्व दृष्टि का परिणाम है। देश के सभी भागों में पर्यावरण के प्रति यही विश्व-दृष्टि दिखाई पड़ती है। तालाब हो या नदी हो, उसे शुद्ध रखने की प्रेरणा हर जगह दिखाई देती है। तालाब के कारण बने मंदिर पर्यावरण के पहरुए बने। ढोर कहां नहाए और आदमी कहां नहाए, इस विभाजन के लिए पंचायत ने कानून नहीं बनाया। मगर स्थान संरक्षित ही रहे। सुदूर केदारनाथ में गया तो वहां मालूम पड़ा कि पुजारी ब्रम्ह कमल लेने गए हैं। यह भी मालूम पड़ा कि वे अपने साथ विविध पूजा सामग्रियों के अलावा कुछ शहद-चीनी भी ले गए हैं। वे तो परंपरा के नाते ले गए मगर अंतर्निहित थी पर्यावरण के प्रति ये दृष्टि कि जितने ब्रम्ह कमल वे तोड़ेंगे उसके कारण वहां के कीड़े-मकोड़ों और शहद की मक्खियों के आहार की क्षतिपूर्ति उसके बदले छींटे गए चीनी या शदहद से होनी ही चाहिए। हल चलाने के पहले धरती की पूूजा आवश्यक है। गोपाष्टमी के दिन गाय बैल की पूजा आवश्यक है। पशुओं को देवताओं एवं देवियों के वाहन बनाकर हमने उनकी पवित्रता को स्वीकार किया है। कौआ, चांद और बंदर आदि से मामा का रिश्ता बनाना और पीपल, बरगद आदि सभी स्थावर जंगम सृष्टि के अंगों के प्रति आत्मीयता और उनके पावित्र्य की मान्यता को स्वीकार करना सामान्य जन की सहज प्रवृत्ति रही है।
हमारा सत्ता प्रतिष्ठान जिस पश्चिमकी नकल करता है, वहां राज्य और व्यक्ति के अलावा किसी अन्य इकाई का समाज संचालन की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। वहा यही दो इकाईयां फल-फूल रही हैं। इसका दुष्परिणाम आज हम सबके सामने है। सत्ता की महत्ता ने उन समाजों को सरकारवाद से जकड़ा जबकि प्रतिक्रिया स्वरूप उपजे व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। इन सबको मिला-जुला परिणाम यह हुआ कि वहां के बूढ़े लोग सरकार के भरोसे छोड़ दिए गए। भारत मे यह जिम्मेदारी परिवार ने संभाल रखी है। इसलिए हमारे यहां सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट का लगभग 3 प्रतिशत पैसा लगता है, जबकि अमेरिका में बजट का 40 प्रतिशत पैदा सामाजिक सुरक्षा में जाता है। यदि भारत के बारे में सोचें तो यहां लगभग 20 करोड़ वृद्ध है जिनमें 10 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। यदि एक-एक को कम से कम गुजर-बसर के लिए हजार रुपये ही दिए जाएं तो 12 हजार रुपये सालाना, उसे 10 हजार भी मान लें तो यदि 10 करोड़ लोगों को साल का 10 हजार रुपये दें तो एक लाख करोड़ होगा। हमारा कुल बजट 8 लाख करोड़ से कुछ ही ज्यादा होता है। इसी में सुरक्षा, उद्योग, कृषि, शिक्षा सब है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत में अमेरिका की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा देना संभव नहीं। बिना किसी सरकारी मदद के यदि भारत के वृद्ध लोग सम्मान पूर्वक जीवित हैं तो इसे परिवार संस्था का चमत्कार ही कहा जाएगा। इस एक उदाहरण से में परिवार संस्था के अमूल्य योगदान की एक झलक मिल जाती है।
भारत में संन्यासी या वानप्रस्थी को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं होता। यहां सामाजिक संरचना की मूल इकाई परिवार है। व्यक्ति और परिवार की चेतना का क्रमिक विस्तार कुटुम्ब, गोत्र, गांव, इलाका, देश, विश्व, ब्रम्हांड और इससे परे के स्तरों पर भी हो जाता है। ये सभी इकाईयां न तो स्वयं में संपूर्ण हैं और न स्वयं में स्वतंत्र हैं। वास्तव में ये सभी इकाईयं अंगांगी भाव से उत्तरोत्तर विकसित हो जाती है। ये इकाईयां अलग-अलग वृत्त नहीं हैं वरन् एक ही चेतना के उत्तरोत्तर विकास की अखंड मंडलाकार व्यवस्था हैं और इसमें परिकर, परिजन, पर्यावरण और परिवेश, जैविक रूप से गुंथे हुए हैं। इन सबमें समन्वय, संतुलन, पारस्परिकता, परस्परावलंबन, सहकार एवं सहयोग को विकास के लिए अपरिहार्य माना गया है। हमारे यहां कभी भी स्पर्धा एवं संघर्ष को विकास का आधार नहीं माना गया। इसे उन्नयन नहीं विकृति एवं अवनति का मार्ग कहा गया है। यहां पश्चिमी समाजों से भिन्न, अधिकार नहीं कर्तव्य के भाव के आधार पर, लाभ-लोभ नहीं प्रतिष्ठा और धर्म के अधिष्ठान पर वंचितों को सहारा और कमजोरों को सशक्त बनाने की विधि निर्मित हुई है। इसके कारण ही जहां पश्चिम में ये नारा लगा कि कमाने वाला खाएगा वहीं भारतीय पंरपरा मंे सुधारा हुआ नारा बना- जो जन्मा है वो खाएगा, कमाने वाला खिलाएगा। इसका तात्पर्य अकर्मण्यता को प्रोत्साहन नहीं मानना चाहिए। मनुष्य कर्म से विरत रहे, यह अपेक्षा हमारे उपनिषद्कारों ने नहीं की, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि मनुष्य कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। इसी प्रकार संग्रह की जगह दान की धारणा को लोगों के मन में स्थापित किया गया। साथ ही समाज में त्यागपूर्वक भोग करने की सलाह दी गई।
भारतीय समाज व्यवस्था में बचत, मितव्ययिता, सादगी एवं अपरिग्रह के जीवन-मूल्य के नाते स्वीकार किया गया है। फिजूलखर्ची या ऐश्वर्य के भौंड़े प्रदर्शन को समाज मं उपेक्षा या निरादर प्राप्त होता रहा है। जो न्यूनतम व्यय करे उसे सर्वाधिक सम्मान प्राप्ति की व्यवस्था समाज में आज भी स्वीकृत है। परिणाम स्वरूप सर्वस्वत्यागी संन्यासी को जो प्रतिष्ठा एवं मान्यता समाज मं प्राप्त होती है वह किसी शक्तिमान या धनाढ्य को नहीं मिलती।
‘इस्तेमाल करो और फेंको’ का सिद्धांत आज की बाजारवादी व्यवस्था में मांग निर्माण हेतु आवश्यक है। लेकिन भारत की आर्थिक सोच इससे अलग रही है। हमारे यहां घर की चीजें फेंकी न जाएं, वे कभी-कभी काम आ जाएं, इसका ध्यान घर में मां आज भी रखती है। खर्च में अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की बजाए बचत एवं मितव्ययिता से पूंजी निर्माण और फलतः समाज में समृद्धि का वितरण हो, यही हमारी दृष्टि रही है। पश्चिम में बैठे कुछ लोग दुनिया के विभिन्न देशों की जी.डी.पी. नापकर उनकी आर्थिक प्रगति या पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। लेकिन उन लोगों को शायद मालूम नहीं कि हमारा देश एक अलग तरह से चलता है। भारत ैसे देश की तरक्की को जी.डी.पी. या ग्रोथ रेट से नहीं नापा जा सकता। जी.डी.पी. नापें भी तो कैसे? हमारे घरों में बहन की डिलीवरी हो तो भाभी को बुला लिया जाता है। मां और भाभीएक माह पहले आ जाती हैं और एक माह बाद तक रहती हैं। वे चूंकि पैसा नहीं लेतीं इसलिए उनके काम को जी.डी.पी. में नहीं जोड़ा जा सकता। अस्पताल या नर्स के काम को भाभी या मां द्वारा कर देने से जी.डी.पी. नहीं बढ़ता है। अगर देश में अपराध बढ़ें, थाना पुलिस के नाम पर पैसा खर्च किया जाए तो जी.डी.पी. बढ़ता है, जबकि सामुदायिक प्रयास या मेलजोल से शांति स्थापित की जाए तो देश का जी.डी.पी. घटता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक नातेदारी का अप्रत्यक्षही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष योगदान भी है। आज भारत के जी.डी.पी. अर्थात सकल उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी औपचारिक क्षेत्र का भाग केवल एक तिहाई है। शेष दो तिहाई भाग भारत के कुटुंबों और उनके सहज समुदायों के उद्यम से आता है। कृषि भी इसी में सम्मिलित है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि श्रमशील भारतीयों की कुल संख्या के 90 प्रतिशत का भरण-पोषण कुटुम्ब एवं समुदाय पर आधारित उद्यमों से ही होता है जिसे देश के कोने-कोने में लोगों ने अपने-अपने ग्राम परिवार एवं समुदाय में उपलब्ध आर्थिक साधनों, तकनीकी दक्षताओं एवं व्यावसायिक वृत्ति का समुचित नियोजन करते हुए स्थापित किया है। देश में आर्थिक दृष्टि से सफल स्थानों का यदि अध्ययन किया जाए तो एक तथ्य नजर आता है कि इन क्षेत्रों के बढ़ाव में सामाजिक व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा है। इनके फलने-फूलने में राजसत्ता की भूमिका नगण्य रही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में शिवकाशी का आतिशबाजी उद्योग नाडार जाति के कारण हुआ। पंजाब में रामगढ़िया जाति के लोगों ने बटाला, अमृतसर और लुधियाना जैसे औद्योगिक शहरों को बढ़ाने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। आगरा का चमड़ा उद्योग जाटवों, अग्रवालों, एवं माहेश्वरी लोगों की मेहनत से आगे बढ़ा है। ये कहानी देश के कोने-कोने में देख जा सकती है। चाहे सूरत में हीरे-जवाहरात की तराशी का काम हो चाहे राजकोट में पंपसेट उद्योग की बात हो, सभी जगह नए लोगों को उद्योग में बढ़ाने के लिए कुटुंब और जाति व्यवस्था में विद्यमान लगाव और आत्मीयता की भावना ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके साथ-साथ अधिक बड़ी पूंजी जातिगत उद्यमिता को समाप्त कर दे या रोजगार मुहैया कराने की इस व्यवस्था को एकाधिकारवादी व्यवस्था निगल न जाए, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो मर्जर, टेकओवर और एक्वीजीशन सरीखी अस्वस्थ वृत्तियां हावी न हो सकें, इस हेतु बचाव की दृष्टि से भी जाति की व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जब हम जाति व्यवस्था या भारत की सामाजिक संरचना की बुराइ्र करने में तल्लीन हो जाते हैं तो हमें इन सकारात्मक पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए।
भारत की सामाजिक संरचना में जातियों की अपनी भूमिका थी । इन जातियों की संरचना ऐसी थी कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से समाज के अन्य जातियों से अविच्छन्न रूप से जुड़े थे। भारतीय समाज में बद जातियों की अपनी एक संस्कृति थी लेकिन संस्कृतियों का विकास इस रूप में था कि किसी अन्य जातियों की संस्कृतियें से भिन्न होते हुए भी इनमें मिश्रित और एकरूप संस्कृति दिखाई पड़ती थी। समाज इन जातियों से अपेक्षा रखता था कि वे इन उच्च उत्तरदायित्वों और समाज के उद्देश्यों को पूरा करें। दूूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इन जातियों के गुण कर्म के अनुसार कार्य विभाजन भी था और समन्वय भी था। यद्यपि जब किसी भी समाज में लक्ष्यहीनता, मूूल्यहीनता, दायित्व बोध की कमी या संकुचित स्वरूप आने लगता है तभी इनके अंतर्विरोध भी धीरे-धीरे क्रमशः संघर्ष का रूप धारण करने लगता है। सत्ता में बैठे लोग इन संघर्षों को हथियार बना अपनी संरचना की कमियों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जबकि मूल कारण संघर्ष का दायित्वबोध, मूूल्यहीनता की कमी और निजी स्वार्थ की अधिकता है। वर्तमान समय में राजनीति मं जातिविहीन समाज की आवश्यकता है। लेकिन आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में जाति एक गुण है। जाति को राजनीतिक उपकरण बनाना एक गंभीर दोष है, ऐसा मानना चाहिए। 70 के दशक के पश्चात् अनेक जातियों के समूहों में अपने परंपरागत अवयवों को संगठित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश प्रारंभ की जाने लगी। उनके अपने देवता, मठ और शिक्षण संस्थाओं ने मूर्त रूप ले लिया। जबकि ये कार्य समाज के विकास में सहायक हैं। लेकिन जब इसका रूपांतरण राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगती है तो यहीं सामाजिक संरचना में अवनत भी प्रारंभ होने लगती है।
भारतीय सामाजिक संरचना के प्रणालियों पर जब उदारीकरण, बाजारवाद भी भोगवादी संस्कृति को यहां के समाज में आरोपित करने का कुचक्र चलने लगा तो वहीं विभ्रम की अवस्था उत्पन्न होने लगी। ऐसी स्थिति में सत्ता में बैठे लोग तथा सत्ता पाने की आांक्षा रखने वाले लोग अपने-अपने मूल्य और मानदंड गढ़ ताल ठोक कर बैठ गए हैं। जिन्हें वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है।
भारतीय संस्कृति भावमूलक, तर्कमूलक और वैज्ञानिक बोध की उच्चतम और श्रेष्ठतम अवस्था से उपजी एक व्यवस्था है। यह हमें सदैव उच्चतम और श्रेष्ठतम रूपों में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ता में बैठे लोग भारतीय समाज की इन बारीकियों को न तो समझते हैं और न ही समझने का प्रयास करते हैं। बल्कि तुच्छ लाभ से पे्ररित होकर गलत परिभाषा गढ़ने का कुचक्र रचते हैं। वे परंपरागत निकाों को बढ़ावा देने और उनमें आवश्यक सुधार करने की बजाए पश्चिमी सोच और ढांचे के अंतर्गत ही समाज संचालन की विधा विकसित करने की कोशिश करते हैं। विगत 60 वर्षों में यही हुआ है और इस कारण सत्ता प्रतिष्ठान की कार्य क्षमता उत्तरोत्तर कम और जनहित के संदर्भ में अप्रासंगिक होती गई है।
(व्यवस्था परिवर्तन की राह) पुस्तक से साभार
