
पौधों और वनस्पति की दुनिया में काम करने वाले जानते हैं कि 16 वीं सदी में पुर्तगाली गार्सिया डि ओर्टा ने पौधों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में एक स्थानीय भारतीय के ज्ञान को दर्ज किया। ये सभी औषधीय पौधे थे। यही ज्ञान बाद में वह यूरोप ले गया। यह जानकारी ‘कॉलोक्युस डॉस सिम्पल्स ई ड्रोसेज ही कॉसस मिडिसनिस द इंडिया’ (भारत के सरल, दवाएं और औषधीय पदार्थों पर संवाद) का प्रकाशन गोवा में 1563 में किया गया। मान लिया गया कि चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले पौधों की खोज उन्होंने की। जबकि वह वास्तव में सिर्फ उनके बारे में लिख रहे थे।
इसी प्रकार की सही तरीके की टिप्पणियां हॉर्टस मालाबैरिकस के बारे में की गई। उनका विवरण भारत में उपलब्ध वनस्पतियों के ज्ञान पर आधारित था। जिसे डच ने वैद्यों से इकट्ठा किया था। इसने 18वीं सदी में कार्ल लिनास को खासा प्रभावित किया। लिनास का हमारे बीच (हमारे विश्वविद्यालयों में) ‘वनस्पति विज्ञान के संस्थापक’ के तौर पर प्रचार किया गया। उनसे पहले के पौधों के इतिहास के ज्ञान और उनके इस्तेमाल को विशेषकर हमारे जैसे देशों के तथाकथित उच्च शिक्षा संस्थानों में नहीं पढ़ाया गया। इसके अलावा नोमेनकल्चर अब लैटिन में शिफ्ट हो गया है, जो लोगों के दिमाग में बिठाता है कि पौधों का शोध और वर्गीकरण विशेष रूप से पश्चिम में किया गया था।
यही कुछ टेक्सटाइल की दुनिया भी हुआ। हम टेक्सटाइल्स के विनिर्माण सहित अन्य तकनीक क्षमताओं की ओर रुख करते हैं। मैंने देखा कि कैसे यूरोप में टेक्सटाइल के निर्माण की कला का विकास उद्यमियों द्वारा भारतीय टेक्सटाइल निर्माण की प्रक्रियाओं और तकनीकों के अध्ययन के बाद ही हुआ। (ज्यादा जानकारी के लिए मेरी किताब डिकोलोनाइजिंग हिस्ट्री देखें।)
वास्तव में अंग्रेज शासकों ने निराशा में स्थानीय उद्योग को खत्म करने के लिए कुछ इलाकों के स्थानीय बुनकरों (और इसी तरह अफ्रीकी देशों के आयरनस्मिथ्स) के अंगूठे तक कटवा दिए थे। यह सिर्फ इसलिए कि वे गुणवत्ता और मात्रा के मामले में प्रतिस्पर्धा में सक्षम नहीं थे। हम स्थानीय डाई (इंडिगो) के बारे में जानते हैं। आज रासायनिक डाइज से ग्रह के इकोसिस्टम पर होने वाले असर को देखने के बाद प्राकृतिक डाइज का दौर लौटने लगा है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय तकनीक की विशेषताओं की जगह कोई नहीं ले सकता।
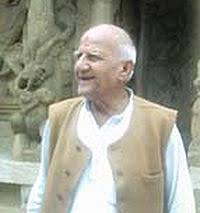
घरेलू फसलों और पशुओं की प्रजातियों की जैव विविधता के रखरखाव में शामिल सजीव सामग्री के साथ तकनीक कौशल का इस्तेमाल भी इसका शानदार उदाहरण है। (चूंकि इसमें भौतिक विज्ञान या गणित या इंजीनियरिंग शामिल नहीं होती है, इसलिए इसे विज्ञान और तकनीक का सामान्य इतिहास नहीं माना जाता है।)
इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदिवासी और खेतिहर किसान ही अकेले धान की 3 लाख प्रजातियों के निर्माण और रखरखाव की समझ रखते हैं। यही नहीं बीज चयन, रखरखाव और संकरण की तकनीक की प्रक्रियाओं का भी वह इस्तेमाल करते थे।
मुझे 1985 में फिलीपींस में आईआरआरआई के भ्रमण के दौरान बात बता चली कि वहां पर धान के 72 हजार अधिकार भारत (भारतीय किसानों की बिना सहमति के) से संग्रिहत की गई थीं। (मेरे ध्यान में ऐसा कोई सामने नहीं आया, जिसने इन ‘कोहिनूरों’ वापस लाने की मांग की हो, जहां से इनकी प्रतियां अमेरिका चली गईं।)
कटक के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में धान की लगभग 60 हजार किस्में हैं, जहां मैं 80 के दशक की शुरुआत में गया था। धान वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. आर एच रिछारिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीटू में धान की 19 हजार किस्मों का रखरखाव किया। आज भी डॉ. देबल देब ओडिशा में अपने अनुसंधान केंद्र बसुधा में चावल की 900 किस्मों का रखरखाव कर रहे हैं। देव ऐसे एक मात्र वैज्ञानिक हैं जो बिना किसी बुनियादी ढांचे के काम कर रहे हैं।
चावल की किस्मों का चयन या उनकी नस्लों में सुधार एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। डॉ. रिछारिया जो खुद दुनिया के अग्रणी चावल प्रजनक हैं, को आदिवासियों की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में अपनी राय बदलनी पड़ी थी जब वह इन किसानों से मिले कुछ बीजों के पुनर्उत्पादन में नाकाम रहे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये प्राकृतिक रूप से मेल स्टराइल लाइन्स थीं। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आदिवासियों को इन किस्मों (जिसके लिए आधुनिक प्रजनक अभी तक जूझ रहे हैं) के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला। लेकिन वे जानते थे कि इन प्राकृतिक किस्मों का क्या महत्व है। इन्हें अपने धान के क्षेत्रों में नई किस्में तैयार करने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह, इनमें से कोई भी कथित ‘सैलीन’ या धान की गहरे पानी की किस्में आधुनिक विज्ञान में तैयार नहीं की गईं। इन्हें तटीय पट्टियों और पानी की कमी वाले क्षेत्रों के किसानों ने चुना, जिससे वे उस जलवायु को अपना सकें।
इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने 50 साल के शोध के बाद आईआर8 और आईआर36 के रूप में महज दो सफलताएं हासिल कीं। बाद मे बीमारियों से पीड़ित हो गईं। इस मामूली सफलता की तुलना ऊपर उल्लिखित हजारों किस्मों से की जा सकती है। अभी तक ये किस्में पूरी तरह से शुद्ध या ‘चुनी गई’ हैं। वे स्थायी किस्म या धारा के ज्ञान या विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। मौजूदा विज्ञान प्रयोगशालाओं से मिली पौध किस्मों का योगदान मौसमी या क्षणिक विज्ञान है, चूंकि उनमें टिके रहने की क्षमता नहीं है, साथ ही कम जेनेटिक आधार के कारण उसकी प्रकृति और प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाता है। अपने दौर में हम बीटी कॉटन के मामले में ऐसा व्यापक स्तर पर होता देख रहे हैं।
इस मानव निर्मित जैव विविधता को कई अन्य फसलों में होता देख रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय किसानों ने बैंगन की 2500 किस्में विकसित की हैं। इसे देश में जेनेटिकली तैयार एगप्लांट को पेश करने के मोनसांटो के प्रस्ताव के खिलाफ किसानों के चर्चित आंदोलन के बाद मान्यता मिली। अब आधार के तौर पर स्वदेशी किस्मों को इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस उत्पाद पर स्वामित्व मोनसांटो का होगा।
 बीज चयन और ऐसे चयन की शुद्धता को बरकरार रखते हुए काम करने की क्षमता के परिणाम स्वरूप उपज बरकरार रही। जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। अलेक्जेंडर वाकर से सर अल्बर्ट हॉवर्ड तक अंग्रेज कृषि विशेषज्ञों की ऐसी कई विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट हैं, जो अंग्रेज किसानों को यह पढ़ाने के लिए आई थीं कि कैसे किसानी की जाए। हालांकि कुछ ही समय में ये बेकार हो गईं, क्योंकि उनमें पढ़ाने के लिए काफी कम था। धर्मपाल द्वारा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स से लिए चिंगलेपट के 18वीं सदी के कृषि उपज से संबंधित आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन आज इस्तेमाल होने वाली हरित क्रांति की सर्वश्रेष्ठ (और सबसे महंगी) फसलों से कहीं ज्यादा था।
बीज चयन और ऐसे चयन की शुद्धता को बरकरार रखते हुए काम करने की क्षमता के परिणाम स्वरूप उपज बरकरार रही। जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। अलेक्जेंडर वाकर से सर अल्बर्ट हॉवर्ड तक अंग्रेज कृषि विशेषज्ञों की ऐसी कई विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट हैं, जो अंग्रेज किसानों को यह पढ़ाने के लिए आई थीं कि कैसे किसानी की जाए। हालांकि कुछ ही समय में ये बेकार हो गईं, क्योंकि उनमें पढ़ाने के लिए काफी कम था। धर्मपाल द्वारा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स से लिए चिंगलेपट के 18वीं सदी के कृषि उपज से संबंधित आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन आज इस्तेमाल होने वाली हरित क्रांति की सर्वश्रेष्ठ (और सबसे महंगी) फसलों से कहीं ज्यादा था।
कपास भी इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे आधुनिक कृषि तकनीकों से मदद मिलने के बजाय हालात और बिगड़ते चले गए। 120 साल पुराने कपास उत्पादन (और यह भी याद रखें कि 1966 से पहले पेस्टिसाइड्स और रासायकनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता था) के आंकड़ों को देखना चाहिए, जो मुझे हाल में झारखंड में इन मुद्दों पर काम कर रहे एक एक्टिविस्ट सौमिक बनर्जी ने भेजेः
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 2013-14 में कपास की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 577 किलोग्राम रही, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा 785 किलोग्राम प्रति हेक्येटर की सबसे ज्यादा उपज रही।
अब सर जॉर्ज वाट की डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम-4 (1890) में उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालते हैं:
1888-1889 के आंकड़ों के मुताबिक हम देख सकते हैं कि भारत के 19 जिलों में स्वदेशी कपास की औसत उपज 577 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा रही है। नीचे तालिका देखें-
1889-90 जिला प्रांत मौजूदा राज्य का हिस्सा उपज-किग्रा प्रति हेक्टेयर काशर असम असम 597 गारो हिल्स असम मेघालय 672 ढोलपुर राजपूताना राजस्थान 718 चिट्टगांव हिल्स बंगाल बांग्लादेश 747 करनाल पंजाब हरियाणा 822 सिंध 6 जिला सिंध पाकिस्तान 824 रोहतक पंजाब हरियाणा 897 अंबाला पंजाब हरियाणा 897 डेरा गाजी खान पंजाब पाकिस्तान 897 रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान 897 जालंधर पंजाब पंजाब 927 गोलपारा असम असम 977 मोंटोगमरी पंजाब पाकिस्तान 1110 मिमेनसिंग बंगाल बांग्लादेश 1779
बनर्जी ने उसी स्रोत से मिलीं कुछ दिलचस्प टिप्पणियों का भी उल्लेख कियाः
‘1870 में गोपालपुर, जौनपुर के श्री जे जी फ्रेजर ने बारिश में हुई बुआई के बाद हिंगनघाट कपास की खेती का भी उल्लेख किया। इस ज्यादा उपज वाले कपास से कुल 1405 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल हुई। ’
‘कानपुर फार्म में एक 2 साल के प्रयोग के बाद अधिकारियों ने सिंचाई के दौरान 635 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और गैर सिंचाई हालात में 561 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज दर्ज की।’
 ‘कपास के स्थानीय रेसेस में सुधार के प्रयासों, कई प्रयोगों से विदेशी बीजों को सिंध की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बनाया गया। नतीजों से साबित हुआ कि सिंधी रेस के साथ कोई भी बीज मिट्टी और जलवायु के स्थानीय हालात के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मुख्य रूप से विदेश में प्रयोग की गई बोरबॉन कपास से सिर्फ 354 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज हासिल हुई, जबकि दूसरी तरफ इसी साल समान हालात में देशी कपास से 1992 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल मिली।’
‘कपास के स्थानीय रेसेस में सुधार के प्रयासों, कई प्रयोगों से विदेशी बीजों को सिंध की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बनाया गया। नतीजों से साबित हुआ कि सिंधी रेस के साथ कोई भी बीज मिट्टी और जलवायु के स्थानीय हालात के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मुख्य रूप से विदेश में प्रयोग की गई बोरबॉन कपास से सिर्फ 354 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज हासिल हुई, जबकि दूसरी तरफ इसी साल समान हालात में देशी कपास से 1992 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल मिली।’
यहां यह दोहराना उचित है कि 2013 की कपास की फसल (औसतः 577 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) रासायनिक उर्वरकों, घातक पेस्टिसाइड्स और सिंचाई के इस्तेमाल के बाद हासिल हुई थी। मोनसांटो ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर कपास के स्थिर उत्पादन का दुरुपयोग किया, साथ ही देश में हर कहीं जेनेटिकल मोडिफाइड कपास को थोपने के लिए कृषि वैज्ञानिक समुदाय का समर्थन हासिल किया। गुजरात जैसे कुछ राज्यों में 90 फीसदी कपास जेनेटिकली मोडिफाइड है, जिसके लिए फिलहाल भारत सरकार से मंजूरी नहीं है।
इसके अजीबोगरीब परिणामों पर नजर डालते हैं: तीन साल पहले जैविक कपास का भारत का 30 फीसदी निर्यात खारिज कर दिया गया और विदेश से वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उसमें बीटी कपास के जीन्स मिले हुए थे। भारत दुनिया में जैविक कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास, जैविक तौर पर पैदा कपास में पाया जाता है तो पूरी खेप जैविक परीक्षण में फेल हो जाती है। जैविक को बढ़ावा देना मौजूदा सरकार की खासी गंभीर चिंता है।
इसके अलावा घरेलू जानवरों के लिए क्षेत्र में हालात खासे बदतर हैं। हमने अभी तक (देर से ही सही) मवेशियों की सिर्फ 39 भारतीय नस्लों को मान्यता दी है। इनमें से अधिकांश नस्लों को न्यूजीलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से आयात की गई हैं, क्योंकि वे बीमारियों को लेकर खासी प्रतिरोधी क्षमताओं से युक्त हैं। इन देशों ने दूध और मांस दोनों के लिए संभावित नस्लों में खासा सुधार किया है। ब्राजील में आज एक गिर गाय रोजाना 60 लीटर दूध देती है। भारत में हमने इसकी पूरी तरह अनदेखी कर दी, इसके बजाय यूरोप से नस्लों का आयात किया। ऐसा शहरी क्षेत्रों के वास्ते त्वरित समाधान पेश करने की सनक के कारण किया गया।
अब मौजूदा सरकार द्वारा पुरानी भारतीय नस्लों को फिर से तैयार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार (बीजेपी) और इजरायल, और भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया ने हाल में भारतीय नस्लों की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विदेशी वीर्य और जमे हुए भ्रूण के आयात के लिए हाल में समझौते किए हैं। इस सनक को समझना खासा मुश्किल है, जो इलाज नहीं है।
इस समाज की जल, जल संरक्षण, जल नौवहन को लेकर पारंपरिक सोच इंजीनियरिंग डिवाइसेस और छोटे स्तर के भंडारण समाधानों से जाहिर होती है, जो राजेंद्र सिंह और अनुपमा मिश्रा जैसे अथक कार्यों के कारण विद्वानों और इंजीनियरों में विकसित हुई है।
बड़े स्तर पर पूरी बारीकी से तैयार सिंचाई व्यवस्था से सिर्फ बड़ी मात्रा (उदाहरणः राजस्थान, पुणे, केरल में कासरगोड की सुरंग परंपराओं जो अरबी दुनिया की क्वांत के समान थीं) में परिवहन और जल भंडारण में ही लोग सक्षम हुए हैं, लेकिन तालाब सिंचाई (उदाहरण के लिए, कर्नाटक) की व्यवस्था को उस समय ठीक से डिजाइन किया गया था जब अंग्रेज इंजीनियरों ने टैंकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया था, तो उन्होंने पाया कि वहां ज्यादा लोकेशन नहीं है, क्योंकि पहले मौजूद तालाबों में बारिश के पानी के संग्रह की पर्याप्त व्यवस्था थी। इस साल मई में मैं 400 साल पहले बनाए गए भूमिगत जल निकास से 1 किलोमीटर तक गुजरा था। इसका इंजीनियर एक मुस्लिम हिंदू था। यह नहर 3 किलोमीटर लंबी थी। ऐसी 6 नहरें पाई गईं। इनमें से एक को बहाल किया जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बार-बार चलने वाले सूखे को देखते हुए भविष्य में जल की स्थायी उपलब्धता के लिए यह इंजीनियरिंग कार्यों के लिहाज से अहम है।
भारतीय जल संचयन प्रणालियों को मानसून को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जो जहां पानी गिरता है वहां संग्रह किया जाता है, जो काफी हद तक मुंबई के औसत नागरिक के समान है, जो सुबह एक घंटे में कंटेनर भर लेते हैं, जब सरकारी पानी की आपूर्ति शुरू होती है और बंद हो जाती है।
गैर मानसून वाले देशों के बांधों की तकनीक पर बन रही आधुनिक सिंचाई प्रणालियां कभी टिकाऊ नहीं रही, चूंकि वे बांध होने वाली बारिश के पूरे पानी को जमा करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा चलने के लिए होते हैं। हकीकत में जो वन काटे जाते हैं और नदी के अपवाह क्षेत्र में पानी जमा होता है, जिससे बांध के जलाशय भर जाते हैं। चूंकि अपवाह क्षेत्र को वनस्पति के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए कटाव और गाद के चलते बांध की उम्र घट जाती है। तालाब सिंचाई प्रणाली में तालाब में जमा गाद को हटाया जाता था और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे तालाब की भंडारण क्षमता बनी रहती है।
