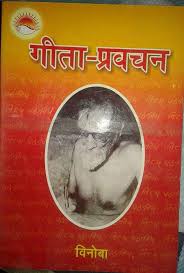 अभी तक हमने अर्जुन के विषाद योग को देखा। जब अर्जुन जैसी ऋजुता(सरल भाव) और हरिशरणता होती है, तो फिर विषाद का भी योग बनता है। इसी को हृद्य-मंथन कहते हैं। गीता की इस भूमिका को मैने उसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन-विषाद-योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद योग जैसा सामान्य नाम दिया है। क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है। यह नहीं समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के पांडुरंग का अवतार सिर्फ पुंडलीक के लिए हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि पुंडलीक के निमित्त से वह हम जड़ चेतन के उद्धार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है। इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त क्यों न हो, हम सबके लिए है। अत: गीता के पहले अध्याय के लिए विषाद योग जैसा सामान्य नाम ही शोभा देता है। यह गीता रूपी वृक्ष यहां से बढ़ते-बढ़ते अंतिम अध्याय में प्रसाद योग रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। ईश्वर की इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावास की मुद्दत में वहां तक पहुंच जाएंगे।
अभी तक हमने अर्जुन के विषाद योग को देखा। जब अर्जुन जैसी ऋजुता(सरल भाव) और हरिशरणता होती है, तो फिर विषाद का भी योग बनता है। इसी को हृद्य-मंथन कहते हैं। गीता की इस भूमिका को मैने उसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन-विषाद-योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद योग जैसा सामान्य नाम दिया है। क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है। यह नहीं समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के पांडुरंग का अवतार सिर्फ पुंडलीक के लिए हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि पुंडलीक के निमित्त से वह हम जड़ चेतन के उद्धार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है। इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त क्यों न हो, हम सबके लिए है। अत: गीता के पहले अध्याय के लिए विषाद योग जैसा सामान्य नाम ही शोभा देता है। यह गीता रूपी वृक्ष यहां से बढ़ते-बढ़ते अंतिम अध्याय में प्रसाद योग रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। ईश्वर की इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावास की मुद्दत में वहां तक पहुंच जाएंगे।
दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा शुरू होती है। शुरू में ही भगवान जीवन के महासिद्धांत बता रहे हैं। इसमें उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। दूसरे अध्याय में आने वाले सांख्य बुध्धि का अर्थ मै करता हूं- जीवन के मूलभूत सिधांत। इन मूल सिधांतों को अब हमें देख जाना है। परंतु इसके पहले यदि हम इस सांख्य शब्द के प्रसंग से गीता के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें, तो अच्छा होगा।
गीता पुराने शास्त्रीय शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त करने की आदी है। पुराने शब्दों पर नये अर्थ की कलम लगाना विचार क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त है। इससे गीता के शब्दों को व्यापक सामार्थ्य प्राप्त हुआ और वह तरोताजा बनी रही, एवं अनेक विचारक अपनी-अपनी आवश्यकता और अनुभव के अनुसार उसमें से अनेक अर्थ ले सके। अपनी-अपनी भूमिका पर से ये सब अर्थ सही हो सकते हैं, और उनके विरोध की आवश्यकता न पड़ने देकर हम स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं। ऐसी मेरी दृष्टि है।
इस सिलसिले में उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार देव,दानव और मानव, तीनों प्रजापति के पास उपदेश के लिए पहुंचे। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया – द। देवों ने कहा हम देवता लोग कामी है। हमें विषय भोगों की चाल लग गई है। इसलिए हमें प्रजापति ने द अक्षर के जरिए दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहाकि हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, इसलिए द अक्षर से प्रजापति ने हमे यह शिक्षा दी है कि दया करो। मानवों ने कहाकि हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीचे पड़े है, हमें द अक्षर से दान करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है। प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना। क्योंकि सभी ने उनको अपने अनुभवों से प्राप्त किया था। गीता की परिभाषा करते समय उपनिषद की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
जीवन सिद्धांत: देह से स्वधर्माचरण
 दूसरे अध्याय में जीवन के तीन महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए है- पहला आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा देह की क्षुद्रता। तीसरा स्वधर्म की अबाध्यता। इनमें स्वधर्म का सिधांत कर्तव्य रूप है। शेष दो ज्ञातव्य हैं। इसके पहले हमने स्वधर्म के बारे में कुछ कहा है। यह स्वधर्म हमे निसर्गत: ही प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे धरती पर संभलें। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था। हमारे मां बाप थे। अड़ोसी पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है। इसलिए जिस मां बाप की कोख से हम जन्में हैं उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मत: ही प्राप्त हो गया है। जिस समाज में मैने जन्म लिया, उसकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम से अपने-आप प्राप्त हो गया। सच तो यह है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है। क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। कोई कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं। कहते हैं कि जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद माना जाता है, वैसे ही यह स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण लगती है। मै स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूं। मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा। वह पहले ही निश्चित हो चुकी हैं। वह कैसी भी क्यों न हों, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानो स्व को ही टालने जैसा आत्मघाती है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अत: यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए – यह जी सब लोग इसी कार्यक्रम वन का मूलभूत सिधांत स्थिर होता है।
दूसरे अध्याय में जीवन के तीन महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए है- पहला आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा देह की क्षुद्रता। तीसरा स्वधर्म की अबाध्यता। इनमें स्वधर्म का सिधांत कर्तव्य रूप है। शेष दो ज्ञातव्य हैं। इसके पहले हमने स्वधर्म के बारे में कुछ कहा है। यह स्वधर्म हमे निसर्गत: ही प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे धरती पर संभलें। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था। हमारे मां बाप थे। अड़ोसी पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है। इसलिए जिस मां बाप की कोख से हम जन्में हैं उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मत: ही प्राप्त हो गया है। जिस समाज में मैने जन्म लिया, उसकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम से अपने-आप प्राप्त हो गया। सच तो यह है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है। क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। कोई कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं। कहते हैं कि जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद माना जाता है, वैसे ही यह स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण लगती है। मै स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूं। मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा। वह पहले ही निश्चित हो चुकी हैं। वह कैसी भी क्यों न हों, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानो स्व को ही टालने जैसा आत्मघाती है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अत: यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए – यह जी सब लोग इसी कार्यक्रम वन का मूलभूत सिधांत स्थिर होता है।
स्वधर्म हमें इतना सहजप्राप्त है कि हमसे अपने आप उसीका पालन होना चाहिए। परंतु अनेक प्रकार के मोहों के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाइ से होता है और हुआ भी, तो उसमें विष – अनेक प्रकार के दोष – मिल जाते हैं। स्वधर्म के मार्ग में कांटें विखेरने वाले मोहों के बाहरी रूपों की तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब हम उनकी छानबीन करते हैं, तो उन सबकी तह में एक मुख्य बात दिखाई देती है – संकुचित और छिछली देहबुद्धि। मै और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बस इतनी ही मेरी व्याप्ति है – फैलाव है, इस दायरे के बाहर जो हैं, वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन हैं – भेद की ऐसी दीवार यह देह बुद्धि खड़ी कर देती है। और तारीफ यह है कि जिन्हें मैं अथवा मेरे मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती है। देह बुद्धि के इस दुहरे पेच में पड़कर हम तरह तरह के छोटे डबरे बनाने लगते हैं। प्राय: सब लोग इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इसमें किसी का डबरा बड़ा तो किसी का छोटा। परंतु है वह डबरा ही। इस शरीर की चमड़ी जितनी उसकी गहराई है। कोई कुटुंबाभिमान का डबरा बनाकार रहता है। कोई देशाभिमान को। ब्राम्हण-ब्राम्हणेत नाम का डबरा है। हिन्दू मुसलमान नामका दूसरा। ऐसे एक-दो नहीं, अनेक डबरे हैं। जिधर देखिए, उधर ये डबरे ही डबरे। हमारी इस जेल में भी तो राजनैतिक कैदी और दूसरे कैदी, इस तरह के डबरे बने ही है। मानो इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। परंतु इसका नतीजा? यही कि हीन विचार के कीड़ों की और रोगाणुओं की बाढ़ आती है। और स्वधर्म रूपी आरोग्य का नाश होता है……………आगे जीवन-सिद्धांत: देहातीत आत्मा का भान..
