 वर्ष 2024 में छपी किताबों की बात करें तो सबसे बड़ी घटना निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह ‘थिगलियाँ’ का आना रहा। इस संग्रह में चार कहानी उनकी मशहूर कहानी संग्रह ‘परिंदे’ से पहले छप चुकी थी। बाकी की कहानियां उनके अंतिम प्रकाशित संग्रह ‘सूखा’ है। कई कहानियां बाद में पत्र-पत्रिकाओं में छपी जरूर, लेकिन कोई और संग्रह नहीं छप सका। अब यह उनका अंतिम संग्रह है। बड़े आदर और सम्मान के साथ राजकमल प्रकाशन ने उनकी सारी किताबों को प्रख्यात चित्रकार रामकुमार के चित्रों के साथ दोबारा प्रकाशित किया है। इसी वर्ष आयी प्रत्यक्षा की नयी किताब ‘अतर : दुनिया में क्या हासिल’ पाठक पढ़ता है तो वह एक नैसर्गिक गद्य पढ़ने के आनंद में डूब जाता है। छह कहानियों के इस संग्रह में दृश्य और अदृश्य को संपूर्णता में उकेरती चलती हैं प्रत्यक्षा, वैसा अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है।
वर्ष 2024 में छपी किताबों की बात करें तो सबसे बड़ी घटना निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह ‘थिगलियाँ’ का आना रहा। इस संग्रह में चार कहानी उनकी मशहूर कहानी संग्रह ‘परिंदे’ से पहले छप चुकी थी। बाकी की कहानियां उनके अंतिम प्रकाशित संग्रह ‘सूखा’ है। कई कहानियां बाद में पत्र-पत्रिकाओं में छपी जरूर, लेकिन कोई और संग्रह नहीं छप सका। अब यह उनका अंतिम संग्रह है। बड़े आदर और सम्मान के साथ राजकमल प्रकाशन ने उनकी सारी किताबों को प्रख्यात चित्रकार रामकुमार के चित्रों के साथ दोबारा प्रकाशित किया है। इसी वर्ष आयी प्रत्यक्षा की नयी किताब ‘अतर : दुनिया में क्या हासिल’ पाठक पढ़ता है तो वह एक नैसर्गिक गद्य पढ़ने के आनंद में डूब जाता है। छह कहानियों के इस संग्रह में दृश्य और अदृश्य को संपूर्णता में उकेरती चलती हैं प्रत्यक्षा, वैसा अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है।
अणुशक्ति सिंह को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। वह ‘शर्मिष्ठा’ के बाद इस वर्ष ‘कित-कित’ उपन्यास में, स्त्री-पुरुष के बीच संबंधों की ऊष्मा कैसे गुम हो रहती है, उस पर बारीक नजर डालती हैं। वह एक ऐसी लेखिका के रूप में उभरी हैं जिनकी नजर अपने दाएं-बाएं देखते हुए स्वतंत्र चलने की हैं। वे उपन्यास में विवरण देने से बचती हैं। उनका ‘देखना’ अपने समकालीन लेखक-लेखिकाओं से अलग और ‘विशेष देखना’ है। सेतु प्रकाशन तसनीम खान का प्रकाशित दूसरा उपन्यास ‘हमनवाई न थी’ शुरू से आखिर तक एक प्रेम कथा है। लेकिन तसनीम खान के इस उपन्यास को ढेर सारी प्रेम कथाओं की कतार में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि यह निरी प्रेम कथा नहीं है, हमारे समकाल में छाये एक खौफ का खामोश प्रतिकार भी है। ‘कोठागोई’ फेम वाले प्रभात रंजन का लोक और व्यंग्य के तुर्श-भीने रंगों में रंजित उपन्यास ‘किस्साग्राम’ का प्रकाशन राजपाल ने किया है। छकौड़ी पहलवान के बहाने यह उपन्यास देश के माहौल पर एक टिप्पणी है।
हिंदी में सबसे ज्यादा किसी विधा में रचनाकार अपने को सहज महसूस करता है तो वह विधा कविता है। सविता सिंह वरिष्ठ कवयित्री हैं। उनके नये संग्रह का शीर्षक ‘वासना एक नदी का नाम है’। इस संग्रह की कविताएं वासना का अर्थ विस्तार करती हैं। यहां वासना सृष्टि का पर्याय है जिसके लिए जिम्मेदारी भरा लगाव जरूरी है। यह आश्चर्य का विषय है कि पचहत्तर साल की उम्र में कवि का पहला संग्रह आये? प्रकाश चंद्रायण, आलोक धन्वा और अरुण कमल की पीढ़ी के कवि हैं, उनके पहले संग्रह का शीर्षक है ‘पददलित मातृभूमि की आत्मा’। पत्रकारिता और कविता का फर्क समझने वाला यह कवि बेहद सजग और सतर्क है, साथ ही बेहद संवेदनशील भी है। कुमार अंबुज की ‘पचहत्तर कविताएं’ संग्रह का चयन-संपादन कवि अरुण देव ने किया। उनका मानना है कि इक्कीसवीं सदी की यातना को जब भी देखा जाएगा कुमार अंबुज की ये चयनित कविताएं याद आएंगी। वे वर्तमान हिन्दी कविता की सबसे विश्वसनीय आवाज हैं। कविताएं कभी भी/ न क्रोध में लिखी जानी चाहिए/ न किसी को क्रोधित करने के लिए, जैसी पंक्तियां चरण सिंह अमी की हैं। वे देवास में रहते हैं। उनके दो संग्रह ‘यात्रा की कविता’ और ‘तानाशाह’ और अन्य कविताएं एक साथ ही अन्य प्रकाशन से छप कर आयी है। विजय देवनारायण साही की कविताओं पर शोध करने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। संजीव कौशल दिल्ली में रहते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे हिंदी में कविता लिखते हैं ‘घर ख्वाबों से बनता है’ उनका नया संग्रह है। छापा संजना बुक्स ने है। उनकी कविताएं वस्तुओं की तरह नहीं मनुष्यों की तरह बात करती है। लोर्का का नाम दुनिया के महान कवियों में लिया जा रहा है। उनकी ‘स्पानी कविताओं का अनुवाद’ वरिष्ठ कवि और प्रो. प्रभाती नौटियाल ने किया है।
फिल्मकार कुमार शहानी का कहना था कि तुकाराम के भीतर इतनी करुणा थी कि वे किसी का भी दुख सह नहीं पाते थे। उनकी कविता सारे देश का दुख, फिर वह शिवाजी के समय का हो या अंग्रेजों की गुलामी का, हर दुख को मिटा देना चाहती थी। उन्हीं तुकाराम की कविताओं का अनुवाद राजेंद्र धोड़पकर ने किया है। ‘तुका आकाश जितना’ इस किताब को रुख पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। युद्ध कहीं भी लड़ी जा रही हो, आहत मनुष्य और मनुष्यता ही होती है। जिल्द बुक्स से प्रकाशित कविता का काम आंसू पोंछना नहीं : प्रतिनिधि फिलीस्तीनी कविताएं संग्रह का संकलन-संपादन पूर्वा भारद्वाज का है। ‘फिलिस्तीन : एक नया कर्बला’ की रचनाओं को लेकर वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा कहती हैं कि मैंने सियासत के साथ समाज को भी रखा है और अपने दुख में आवाम के दुख को देखा है। साहित्य को इसलिए रखा है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके।
भारतीय संस्कृति से गहरे जुड़े श्यामसुंदर दुबे के संस्मरणों का संग्रह है—’ताकि सनद रहे’। इन संस्मरणों में कुछ ऐसे समर्थ चिंतक, कलाविद और कलाकार हैं, जो हमारे वर्तमान में साथ हैं। वागीश शुक्ल जिस परंपरा के उद्भट विद्वान हैं, वह विलुप्त होती हुई परंपरा है। इसलिए हाल ही में प्रकाशित उनकी किताब ‘आहोपुरुषिका’ पर मृदुला गर्ग के ब्लर्ब का एक अंश देने के लोभ से अपने को बचाना मुश्किल है—’मेघदूतम्’ को छोड़ दूं तो पत्नी के वियोग में इतना झंझावाती विषाद, आहोपुरुषिका के अलावा किसी कृति में नहीं देखा। पीड़ा नहीं, विषाद। पीड़ा तो रोजाना का देह व्यापार है, वह भाव नहीं जो मन प्राण को खाली कर दे। कह सकते हैं कि मेघदूतम् में विषाद का मूल तत्त्व काम था। पर वागीश जी ने भी काम को ही प्रणय का मूल उद्गम और विलय बतलाया है। जिस विषाद को इस कृति (झंझावाती खेल) में अभिव्यक्ति मिली है, अमूमन वह तभी हमारे ऊपर सवारी करता है, जब युवा सन्तान, बेटा/बेटी हमारी आँखों के सामने महाप्रयाण कर जाए। उस विषाद में अपराध बोध शामिल रहता है, लाख कोशिश पर अपनी कोई गलती याद न आए तब भी। दरअसल, अपराध बोध होता है, अपने जीवित रह जाने का। और उसका कोई प्रतिकार है नहीं। ऐसे आहोपुरुषिका एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है ‘वह जो दो व्यक्तियों के लिए एक ही समय में उपयोग किया जाता है’।
वह विलुप्त होती हुई परंपरा है। इसलिए हाल ही में प्रकाशित उनकी किताब ‘आहोपुरुषिका’ पर मृदुला गर्ग के ब्लर्ब का एक अंश देने के लोभ से अपने को बचाना मुश्किल है—’मेघदूतम्’ को छोड़ दूं तो पत्नी के वियोग में इतना झंझावाती विषाद, आहोपुरुषिका के अलावा किसी कृति में नहीं देखा। पीड़ा नहीं, विषाद। पीड़ा तो रोजाना का देह व्यापार है, वह भाव नहीं जो मन प्राण को खाली कर दे। कह सकते हैं कि मेघदूतम् में विषाद का मूल तत्त्व काम था। पर वागीश जी ने भी काम को ही प्रणय का मूल उद्गम और विलय बतलाया है। जिस विषाद को इस कृति (झंझावाती खेल) में अभिव्यक्ति मिली है, अमूमन वह तभी हमारे ऊपर सवारी करता है, जब युवा सन्तान, बेटा/बेटी हमारी आँखों के सामने महाप्रयाण कर जाए। उस विषाद में अपराध बोध शामिल रहता है, लाख कोशिश पर अपनी कोई गलती याद न आए तब भी। दरअसल, अपराध बोध होता है, अपने जीवित रह जाने का। और उसका कोई प्रतिकार है नहीं। ऐसे आहोपुरुषिका एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है ‘वह जो दो व्यक्तियों के लिए एक ही समय में उपयोग किया जाता है’।
भारत में अधिकांश समाज वैज्ञानिक लेखन अंग्रेजी में होता है- इसलिए वे तमाम मुहावरे जो दुनिया को देखने की अंग्रेजी भाषी देशों की नजर को अभिव्यक्ति देते हैं, भारतीय समाज वैज्ञानिक लेखन में शामिल हो गये हैं। इसके बावजूद यह कहना लाजिमी है कि अभी भी समाज विज्ञान से जुड़ी अच्छी किताब अनुवाद होकर ही हिंदी में आती है। इन्हीं किताबों में से एक प्रो. राजीव भार्गव की ‘बिटवीन होप एंड डिस्पेयर’ का हिंदी अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने ‘राष्ट्र और नैतिकता’ शीर्षक से किया है। इस किताब में अभिव्यक्त विचारों की टेक ‘राजनीति’ नहीं है, ‘मूल्य’ है। वर्तमान समय में ‘मूल्य’ शब्द व्यापक और अर्थपूर्ण के साथ विवादास्पद भी है, जितना ‘सत्य’ शब्द। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। इसी तरह नैतिक और सामाजिक मूल्य (व्यक्ति की दृष्टि में भिन्न होते हुए भी) नैतिक और सामाजिक मान्यताओं और विश्वासों का एक ऐसा जामा पहन लेते हैं, जो उन्हें स्थूल दृश्य रूप देता है। जमाने के अनुसार ये मान्यताएं बदलती रहती हैं, और यह भी ठीक है कि इन मान्यताओं को बदलने के लिए शक्ति, साहस और सूझ बरकरार होती है।
वर्तमान कितना भी चमकीला हो मानव स्वभाव है कि वह अंधेरे की तुलना व्यतीत समय से करता है। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास के सबसे अंधेरे पलों में से एक आपातकाल का प्रभावी और प्रामाणिक अध्ययन जो हमारे वर्तमान दौर में, लोकतंत्र पर मंडरा रहे वैश्विक संकटों पर भी रौशनी डालता है। वह किताब है ज्ञान प्रकाश की ‘आपातकाल आख्यान’। इस किताब का मूल तर्क है कि आपातकाल के लिए जितनी जिम्मेदार इन्दिरा गांधी थीं, उतने ही जिम्मेदार भारतीय लोकतंत्र और लोकप्रिय राजनीति के बनते-बिगड़ते नाजुक संबंध भी हैं। यह विडंबना ही है कि आज भी हम लोकप्रिय राजनीति से ही ग्रस्त हैं। इस साल रामचन्द्र गुहा की किताब ‘सभ्यता के कोने : वेरियर एल्विन और भारतीय आदिवासी समाज’ को प्रकाशित कर सेतु प्रकाशन ने महत्त्वपूर्ण काम किया है। हिंदी अनुवाद में मूल अंग्रेजी में लिखे का यह संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण है, अनुवाद भी सुंदर है।
यह सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत-विभाजन के संदर्भ में अपनी भूमिका के लिए निंदित और प्रशंसित दोनों रहे हैं। सेतु से प्रकाशित इश्तियाक अहमद की किताब ‘जिन्ना : उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में भूमिका’ आलोक और अलका बाजपेयी द्वारा अंग्रेजी से अनूदित है। भारत-विभाजन की परिस्थितियों को लेकर गहरी रुचि रखने वालों पाठकों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण किताब है। मैनेजर पाण्डेय अपने अंतिम दिनों में भारत की संगम-संस्कृति के सूत्रों के अध्ययन-अन्वेषण में लगे थे। ‘दारा शुकोह : संगम-संस्कृति का साधक’ किताब उनके इसी साधना का परिणाम है।
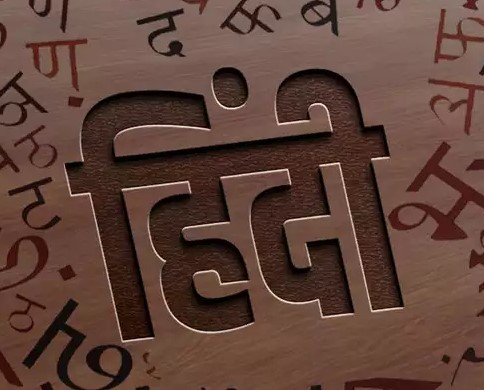 युवा मीडिया विश्लेषक विनीत कुमार की दूसरी किताब ‘मीडिया का लोकतंत्र’ है। विनीत का मानना है कि मीडिया के चरित्र को 2014 के बाद से बदलने की बात करना महज एक सपाटबयानी होगी जबकि इसे पहले से बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदी युग्म से प्रकाशित प्रमोद सिंह की किताब ‘बेहयाई के बहत्तर दिन’ एक सफरनामा है। यह सफरनामा आधुनिक चीन के बारे में नयी जानकारियों से परिचित तो कराता ही है, साथ ही यात्रा पर निकलने को प्रेरित भी करता है। हंस पत्रिका के शुरुआती सालों में प्रकाशित श्रृंखला ‘अभी दिल्ली दूर है’ में अपने समय के आठ नामचीन साहित्यकारों ने लिखा था। यह दिल्ली आजादी के बाद बदलती दिल्ली थी। इस किताब के संपादक रविकांत की प्रतिक्रिया है दिल्ली एक युटोपिया, छलावा, भ्रम और मरीचिका-जैसी लगती है, जहां आकर भी कोई कहीं पहुंचा हुआ महसूस नहीं करता, यहां बसकर भी घर की कसक और लौट जाने की उम्मीद पाले जीवन गुजार देता है। जयशंकर संवेदनशील कथाकार हैं। उनकी किताब ‘कुछ दरवाजें, कुछ दस्तकें’ की भाषा बेहद संवेदनशील और प्रवाह इतना प्रांजल है कि पूरी पुस्तक को एक सांस में पढ़ लिया जा सकता है।
युवा मीडिया विश्लेषक विनीत कुमार की दूसरी किताब ‘मीडिया का लोकतंत्र’ है। विनीत का मानना है कि मीडिया के चरित्र को 2014 के बाद से बदलने की बात करना महज एक सपाटबयानी होगी जबकि इसे पहले से बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदी युग्म से प्रकाशित प्रमोद सिंह की किताब ‘बेहयाई के बहत्तर दिन’ एक सफरनामा है। यह सफरनामा आधुनिक चीन के बारे में नयी जानकारियों से परिचित तो कराता ही है, साथ ही यात्रा पर निकलने को प्रेरित भी करता है। हंस पत्रिका के शुरुआती सालों में प्रकाशित श्रृंखला ‘अभी दिल्ली दूर है’ में अपने समय के आठ नामचीन साहित्यकारों ने लिखा था। यह दिल्ली आजादी के बाद बदलती दिल्ली थी। इस किताब के संपादक रविकांत की प्रतिक्रिया है दिल्ली एक युटोपिया, छलावा, भ्रम और मरीचिका-जैसी लगती है, जहां आकर भी कोई कहीं पहुंचा हुआ महसूस नहीं करता, यहां बसकर भी घर की कसक और लौट जाने की उम्मीद पाले जीवन गुजार देता है। जयशंकर संवेदनशील कथाकार हैं। उनकी किताब ‘कुछ दरवाजें, कुछ दस्तकें’ की भाषा बेहद संवेदनशील और प्रवाह इतना प्रांजल है कि पूरी पुस्तक को एक सांस में पढ़ लिया जा सकता है।
अभी तक हिंदी के लेखकों की जितनी भी जीवनियां आई हैं उनमें मुक्तिबोध की जीवनी ‘मैं अधूरी दीर्घ कविता’ विपुल पृष्ठों में समायी हुई है। मुक्तिबोध के जीवन से जुड़े छोटे-छोटे विवरण यहां मौजूद हैं। मुक्तिबोध ने न भाग्य की चिन्ता की, न भवितव्य की। वह एक स्वप्न के चरितार्थ होने की प्रतीक्षा में जी रहे थे, यह जानते हुए भी कि उनके जीवन-काल में यह सम्भव न होगा। वह संभव नहीं हुआ, और अंधेरा और बढ़ चला है। संभावना प्रकाशन ने ‘अपराजित : शिल्पकार हिमा कौल’ ऐसे कलाकार की जीवनी है जिसे अपनी सारी संभावनाओं को अमलीजामा पहनाने का मौका नहीं मिला। संवेदनशील शिल्पकार की जीवनी को लेखक राजाराम भादू लिखा है। स्वामीनाथन अपने समय के बड़े चित्रकार थे। उनके सान्निध्य में रहने-देखने का मौका चित्रकार अखिलेश को मिला। ‘के विरुद्ध, स्वामीनाथन : एक पक्ष’ उन्हीं की लिखी किताब है। इस किताब के जरिए हम सिर्फ स्वामीनाथन को ही नहीं जानते-समझते, बल्कि उनके समकालीन चित्रकारों की दुनिया से भी परिचित होते हैं।
देवेंद्र राज अंकुर की पुस्तक ‘रचना प्रक्रिया के पड़ाव’ नाटक और रंगमंच के छात्रों, शोधार्थियों और रंगकर्मियों के लिए बेहद महत्त्व है। कम से कम उन्हें कहानी का रंगमंच से संबंधित सारी जानकारियां एक जगह मिल जाती है। मिथलेश शरण चौबे के विचार, लेख व समीक्षाओं के एकत्रण का नतीजा है—’अकथ का आकाश’। यह किताब उन युवा समीक्षकों और आलोचकों को पढ़नी चाहिए जो साहित्य को सह्रदय मस्तिष्क से पढ़ना चाहते हैं। भारत भूषण उपाध्याय पेशे से पशु चिकित्सक हैं और साहित्य के अनुरागी पाठक हैं। ‘साक्षात्कार से साक्षात्कार’ उनके लिखे निबंधों का संग्रह है। इस किताब को उन विषयों पर केंद्रित किया गया है जिसकी गहरी, विस्तृत और उस विषय संबंधित हाल की जानकारियां हिंदी में बहुत कम मिलती है। सतीश कुमार राय ने हमारे पुरखे साहित्यकारों, विद्वानों और पत्रकारों के योगदान को ‘हिंदी-पत्रकारिता के प्रतिमान’ में जिक्र किया है, दिल्ली केंद्र से दूर रहते हुए सतीश जी का यह काम बेहद महत्त्वपूर्ण है। बाबूराव विष्णु पराड़कर के बारे में लिखते हैं कि वे हिन्दी के उन स्वनामधन्य पत्रकारों में अग्रगण्य हैं जिन्होंने अपनी साधना से पत्रकारिता को दीप्त किया, अपने संघर्ष से उसे जिजीविषा दी और अपने संकल्प से उसे नया दृष्टिबोध दिया। पराड़कर जी की पत्रकारिता सर्जनात्मकता की एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक उपलब्धि है, जिसमें प्रखर कालबोध है और व्यापक सन्दर्भों की प्रस्तुति भी। ऐसे अनेक महापुरुषों से पाठक का परिचय होता है।
हिंदी में बच्चों के लिए बहुत ही कम लिखा जाता रहा है। ‘नाम है उसका पाखी’ एक उपन्यास है, लिखा उदयन वाजपेयी ने है। बच्चों की कल्पनाशीलता का परिसर और भी विस्तृत हो, इसमें तापोशी घोषाल के चित्र मदद करते हैं। एकलव्य और अंकुर की साझेदारी में छपी किताब एक शहर एक पहाड़ एक मोहल्ला को फिक्की के पब्लिकेशन 2024 के चिल्ड्रेन्स बुक ऑफ द ईयर- हिंदी केटेगरी में सर्वश्रेष्ठ किताब से नवाजा गया है।
(युगवार्ता से साभार)
